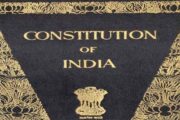महेश पंत
आज सुबह मेरी पिचासी वर्षीय माँ और मैंने हमारे प्रारंम्भिक जीवन के बारे में बातें की। बातें करते करते, पुरानी यादों की लहर सी मन मष्तिष्क पर छा गई। हमारा गाँव नेपाल से भारत की सीमा बनाने वाली काली नदी से मात्र आठ मील की दूरी पर पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। वहाँ के सभी गांवों की तरह हमारा गाँव भी सघन वन आच्च्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घाटी में स्थित है। मीलों तक फैले हुए खेतों के मध्य में घरों का एक समूह है, हमारा गाँव।हरे भरे पहाड़ों और खेतों के बीच में मेरा बचपन बीता। नित्य चिड़ियों की चहचहाहट और नदी की कलकल कल कल ध्वनि से सूर्य की किरणों का स्वागत होता और झींगुरों का सामूिहक स्वर और वन से घर को लौटते हुए पशुओं के धूल उड़ाते झुण्ड शाम की घोषणा करते।
जीवन इतना आसान नहीं था। खेती से मुश्किल से ही परिवार का भरण पोषण हो पाता था। थोड़ा बहुत फल सब्जियां भी हो जाती थी। मवेशी हमारे जीवन का अभिन्न अंग थे जो गोरस और खाद दोनों देते थे। सरकारी योजना ने कभी कभी मुर्गी पालन और उन्नत किस्म के पशुओं की व्यवस्था की और इस सब के बीच जंगल हमारे जीवन के आधार होते थे। इससे हम जलाऊ लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी और औषधीय जड़ी बूटियाँ पाते थे। जंगली फल जैसे काफल और आंवला , जिनकी मीठी खटास आज भी मेरे मुँह में पानी ले आती है ,भी वन से ही मिलते थे। गांव के लोग हर पेड़ और झाड़ी को नाम से जानते थे। वन हमारे मित्रों की तरह थे, यहाँ तक भी कहा जाता है कि वन गाँव की महिलाओं के मायके की तरह होते हैं। वन संपदा का सुरुिचिपूर्ण, समुचित और न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा कार्य करती थी। सच कहूं तो ग्रामीण जीवन मनुष्य – मवेशी और जंगल के संतुिलत संबंधों से पुष्पित, पल्लवित होता था।
आज की स्थिति जीवन एक अलग ही कहानी बताती है। लोग बड़ी संख्या में गांवों को छोड़कर देश के अन्य भागों की ओर पलायन कर चुके हैं। जो गाँव में बचे हैं वह अब खेटी- किसानी नहीं करते, मवेशियों की संख्या बहुत कम रह गई है। यह केवल मेरे गाँव की कहानी नहीं, समूचे उत्तराखण्ड की बात है। मैंने अपनी माँ से कुमाऊँनी में पूछा कि लोग अब खेती क्यों नहीं करते ? “ गुना बानर के राखनै नै, इजा “ (बंदर और लंगूर सब कुछ नष्ट कर देते हैं, बेटा ). उनके उत्तर में अथाह पीड़ा थी।
वास्तव में ग्रामीण जीवन में मानव – मवेशी और जंगल का जो संतुलन पहले अनवरत बना हुआ था , अब डगमगाकर अस्थिर हो गया है।अब लोग अपनी और मवेशियों की आवश्यकताओं के लिए जंगल से चारा और लकड़ी इत्यादि लेने नहीं जा सकते। फलस्वरूप वनस्पितयों की अधिकता हो गई है, वन सघन हो गए हैं और वन्यजीवों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो गई है। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अब वह वन से बाहर निकलकर गाँव और खेतों तक आने लगे हैं । इस दुष्चक्र ने पूरे उत्तराखंड को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और खेती तथा पशुपालन को लुप्तप्राय बना दिया है। यहाँ तक कि कई बार ग्रामीण भालू , चीते और बाघ जैसे जानवरों के गाँव में आने की आशंका से डरे रहते हैं।
मेरे बचपन में राज्य में भौतिक विकास एक सपना सा था। बिजली के बारे में तो सुना ही नहीं था और हमारे गांव में पानी तब पहुँचा जब में तेरह साल का था। तब तक हम पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलते थे। यह रोज़ का संघर्ष हमारी सहनशीलता की परीक्षा थी। मोटर चलने लायक सड़क तब बनी जब मैं 17 साल का हो गया। उससे पहले हमारी जीवनरेखा एक संकरी घोड़ा रोड थी जिस पर सामान, और आपातकाल में, इंसान भी घोड़े पर सवार होकर जाते थे।
अभावों के बीच एक ही आशा की किरण थी- शिक्षा, जो हमारी साधना का माध्यम थी। सरकारी नौकरी को अंतिम आकांक्षा माना जाता था वह हर नौजवान का सपना होती थी। इसके लिए नौजवान कड़ी मेहनत करते और प्रदेश में या देश भर में जहाँ भी अवसर मिलते प्रयास करते। कई लोगों ने – जिनमें मैं भी शामिल हूँ – इस सपने को पूरा किया। सेना, सरकार और अन्य क्षेत्रों में करियर बनाया। उत्तराखंडियों ने सरकारी कायार्लयों से लेकर वैिश्वक निगमों तक, अनेकानेक क्षेत्रों में अप्रतिम सफलता प्राप्त की है और अथक परि श्रम से अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाई है।
आज पहाड़ों में जीवन कहीं ज़्यादा आरामदायक है। पलायन करने वालों से मि लने वाले और सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले पैसे से चलता अथर्तंत्र। घर मज़बूत हैं, सड़कें पक्की हैं और हर घर में बिजली और पाइप से पानी की सुविधा है। एलपीजी ने जलाऊ लकड़ी की जगह ले ली है और आधुिनक उपकरणों, वाशिंग-मशीन, गीजर, टीवी-, ने रोज़मर्रा की ज़िन्दगी को नया आकार दिया है। आज कोई भी बच्चा “ खेत के नीचे एक फ्रिज ” की खोज करने के मासूम आश्चर्य का अनुभव नहीं करेगा, जैसा कि एक बार शहर से आई एक अबोध बालिका ने ठंडे झरने के पानी का स्वाद चखने के बाद कहा था। लेकिन जैसे-जैसे हम आधुिनिकता को अपना रहे हैं, हमने क्या पीछे छोड़ दिया है? स्थानीय रूप से उगाए गए, ज़ैविक-अनाज, दालें और स्वाद और सुगंध से भरपूर फल खाने का विशेषाधिकार गायब हो गया है। भूमिगत झरनों से नि कलने वाला गर्म, खनिज युक्त पानी, घर में उगाई जाने वाली मौसमी सब्ज़ी, वि शेष पहाड़ी फसलों के बने व्यंजन। ठंडी रातों में आग के चारों ओर इकट्ठा बैठकर बातें करने की सरल खुशियाँ , ये ख़ज़ाने पैसे के हस्तांतरण की डिजिटल चकाचौंध में चुपचाप खो गए हैं। इससे भी बदतर यह है कि अब ग्रामीण जंगली जानवरों के डर में जी रहे हैं. कभी-कभी तो उन्हें अपने घरों के पास तेंदुए और भालू का भी सामना करना पड़ता है।
यह सवाल बड़ा है: क्या प्रगति की कीमत, संतुलित जीवन शैली का त्याग होना चाहिये ? अगर समृद्धि को सिर्फ वित्तीय लाभ और बुनियादी ढांचे से परिभाषित किया जाए, तो हाँ, उत्तराखंड प्रगति कर रहा है। लेकिन क्या हमें अपनी ज़मीन की उत्पादक क्षमता को खो देना चाहिये जिससे हमारे पुश्तैनी खेत जंगल बन जाएँ ? वैदिक श्लोक “माता भूमि: , पुत्रोहम पृिथव्या:” (धरती हमारी माँ है, और हम उसके बच्चे हैं) खोखला साबित हो रहा है। क्या अब हम उस मिट्टी की उपेक्षा करें जिसने कभी हमें सहारा दिया था? जो लोग नौकरी नहीं पाते, वे अपना भरण-पोषण कैसे करेंगे ? यह दुविधा केवल नीति-निर्माताओं के सामने ही नहीं बल्कि नागरिकों, सामाजिक संगठनों और सरकारों के भी सामने समान रूप से है। क्या हम ऐसा संतुलन बना सकते हैं जहाँ विकास हमारी सांस्कृतिक और पप्राकृतिक विरासत को खोने की कीमत पर न हो? सरकारी योजनाएँ अक्सर इन समस्याओं को कम करने के बजाय और बढ़ा देती हैं। शायद असली चुनौती ऐसे समाधान तैयार करना है जो खोए हुए संतुलन को बहाल करे, न कि उसे और बिगाड़े। समय आ गया है कि हम बहुत देर होने से पहले एक सार्थक चर्चा शुरू करें। अन्यथा,उत्तराखंड एक ऐसी भूमि बनने का जोखिम उठा रहा है जहाँ न तो परंपरा रहेगी और न ही प्रगति. रह जायेगा खोया हुआ एक स्वर्ग।