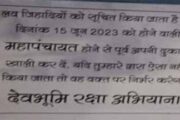राजेन्द्र भटृ
नक्कारखाने में तूती – 6
लंबे अंतराल तक किसी अनिष्ट की आशंका जैसी जड़ता-हताशा मन पर छाई थी। मित्र लोगों की प्रेरणा, दिलासों और फिर थोड़ा चिढ़े हुए उलाहनों के बावजूद नहीं टूटी; फिर अपने ही दौर में जो अनहोनी बदी थी – हो ही गई। अंधे उन्माद और स्वार्थ के सौदागरों की प्रयोगशालाओं और जुबानों से तेजाब-गोबर वाली खादों का जो सैलाब निकला, उससे दिल्ली में आखिरकार दंगों की खूनी फसल लहलहा उठी। गांधी होते तो देशद्रोह के आरोपों और जान का खतरा झेलते हुए चाँदपुर-ज़ाफराबाद-शिवविहार पहुँच जाते पर उनके कथित वारिसों ने आँख-कान बंद कर भयावह कायरता दिखाई। वैकल्पिक राजनीति की झाड़ू भी बेशर्म मुस्कराते गुलदस्तों में तबदील हो गई – और घरों-गलियों-नालों में बेआसरा लाशें पड़ी रहीं, यतीम लहू बहता रहा। इस नरमेध यज्ञ में अंतिम बलि की रस्म पूरी करने के लिए अतिरिक्त ईमानदार नेता ने ‘अपनों’ के लिए ‘अतिरिक्त’ सज़ा की पेशकश की, जो देर-सबेर, देशप्रेम की बलिवेदी पर, कानून से भी ऊपर ‘राष्ट्रीय अंतरात्मा’ की आवाज़ को खुश करने के लिए अदालत दे ही देगी।
जड़ता को तोड़ कर फिर से लिखने की जुगत कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ‘पर्सनल’ होना क्षमा करें। तमाम दर्दों के बीच अचानक गर्दन का दर्द परेशान करने लगा। दरअसल जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हमारा सार्वजनिक चेहरा लोगों को ही नहीं, खुद को भी धोखा देने लगता है। अपने ही झूठ,छल-प्रपंचों का खुद ही मुरीद होने लगता है और खुद को भी सच्चा लगने लगता है। मसलन कब्रिस्तान-श्मशान-पोशाक से हुए बँटवारे की फसलें काट कर अचानक किसी होनहार दलित युवा की आत्महत्या पर टीवी के आगे या जनसभा में गला-आँखें भर आना; माँ-बेटे के स्नेह के नितांत निजी क्षण हों या एकांत में की जाने वाली ‘फिटनेस’ की कसरतें हों – उन्हें कैमरों के बेहतरीन एंगल्स से प्रदर्शित करना वगैरह।
सार्वजनिक जीवन में भी अपने निजी चेहरे की निरंतर पड़ताल करते रहने की नैतिकता और निजी जीवन में भी सार्वजनिक प्रदर्शन के पाखंड के खतरे को बखूबी समझा था नेहरू जी ने। 1937 में तीसरी बार ( 1929 तथा 1930, 1936,1937) काँग्रेस अध्यक्ष ( तब इस बेहद सम्मानित और जन-प्रिय पद को ‘राष्ट्रपति’ कहा जाता था ) चुने जाने के बाद उन्होंने ‘चाणक्य’ उपनाम से एक लेख लिखा जो ‘राष्ट्रपति’ शीर्षक से कोलकाता की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका ‘मॉडर्न रिव्यू’ में छपा। लेख में नेहरुजी ने बेहद लोकप्रियता और जल्दी परिवर्तन लाने की बेचैनी में खुद (नेहरू जी) के अहंकारी तानाशाह बनने की आशंका का आत्म-विश्लेषण किया था और जनता को आगाह किया था कि उन्हें ज्यादा सिर न चढ़ाए, नियंत्रण में रखे। उसी लेख में नेताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण कसौटी को नेहरू ने इन गहन शब्दों में व्यक्त किया – ‘प्राइवेट फेसेस इन पब्लिक प्लेसेस आर बैटर एंड नाइसर दैन पब्लिक फेसेस इन प्राइवेट प्लेसेस ।‘ यानि सार्वजनिक जीवन में भी अगर सामान्य मानवीय कमियों-अच्छाइयों वाला निजी-स्वाभाविक चेहरा सामने आ जाए तो बेहतर है – बनिस्बत इसके कि निजी जीवन के क्षणों में भी अपने सार्वजनिक ‘पाखंडी’ मुखौटे को ओढ़े रखा जाए। पर वो तो नेहरू और नेहरू की पीढ़ी थी नैतिक और बौद्धिक पैमाने पर कद्दावर नेताओं की। आत्म-मुग्धता वाले नकली नैतिक विलाप की सार्वजनिक उल्टियाँ करने का दौर नहीं था वह।
दर्द शारीरिक हो या अपने किए छल-कुकर्मों का धिक्कार हो – उसकी असली तकलीफ होती है रात में नींद आने ( बल्कि नींद न आ पाने) से पहले के क्षणों में – जब तमाम सत्ता, धन, पाखंड, बड्बोलेपन, तिकड़म, क्रूरता के बावजूद हर कोई आम, गरीब जन जैसा ही असहाय, अकेला होता है और सबसे बड़े सुकून से वंचित हो जाता है जिसे कोई सत्ता-धन-तिकड़म-क्रूरता-उन्माद नहीं खरीद सकते – यानि नींद का मलहम, नींद का सुकून।
बहरहाल, नींद से पहले के अंधेरे पलों में, शारीरिक दर्द को, मैं धोखा नहीं दे पा रहा था। नींद नहीं आ रही थी; और जैसा आपको भी अनुभव होगा, आँखों के आगे कई बेतरतीब बिम्ब बेचैनी बढ़ा रहे थे।
एक बिम्ब आया कि बालियाँ पकने से पहले की गेहूं की खड़ी फसल फैलते धुएँ और लपटों में झुलस रही है। धीरे-धीरे झुलसती जीवन की हरी आभा, संभावना, तरलता—-और फिर धुएँ के विस्तार के साथ दूर तक फैले दूसरे खेतों का बिम्ब। —-यहाँ खड़ी फसल जरा भी नहीं है। यहाँ, बस पराली वाली ठूँठें हैं – फिर दूर, जहां तक नज़र का क्षितिज है, ठूँठे तनों का फैलाव है। धुवाँ-लपट यहाँ भी है पर झुलसती फसल के विपरीत, ठूँठों पर इसका कोई असर नहीं पड रहा- कोई तरलता, कोई सौंदर्य — कोई आस नहीं।
बेतरतीब होती है ऐसी तंद्रा – मुझे कुरूप ठूँठों के आकार सिर पर पटके बांधे, मुट्ठियाँ भींचे, कट्टे-बल्लम लिए युवाओं में बदलते दिखे। तो क्या इस हरी-भरी फसल में संभावनाओं की – कला-संस्कृति-प्रेम-विज्ञान-समृद्धि की बालियाँ नहीं पनप सकेंगी? ये बरगलाए-अभागे घृणा-मूढ़ता की आग में यों ही झुलस जाएंगे! और फिर इन पर किसी मौत-तकलीफ-दर्द या सुंदर सपने का असर पड़ना बंद हो जाएगा? ये सुनहरी बालियों-सी उम्मीद भरी पीढ़ी किसी की राजनीति की ठूंठ-पराली बन जाएगी!! क्या इन्हीं पीढ़ियों के लिए, एक पीढ़ी तूफान से किश्ती निकाल लाई थी?
फिर मुझे ख्याल आया कि शिखर पर जमे महामानवों को भी तो नींद आने ( या न आने) से पहले का वक्त अकेले ही काटना पड़ता होगा। लुटयेन दिल्ली ( जिसे हमारे सभी महामानव अपने सार्वजनिक मुख से एकदम पराया बताते हैं, पर रहते वहीं हैं) के ज़बरदस्त सुरक्षित भवनों में, जहां परिंदा भी पर न मार सके, वहाँ भी नींद से पहले आँखों के आगे फड़फड़ाते परिंदों को भला कौन रोक सकता है? कभी 1984, तो कभी 2002 और अब 2019 के असहाय परिंदे घायल पंख फड़फड़ाते होंगे। उन्मादी आतंक के आगे डरी, फटी-फटी आँखें; सुनवाई पूरी कर पाने से पहले ही मर गया कोई न्यायाधीश; पाबंदियों के लंबे दौर की वजह से इलाज के बिना मर गए मरीज; किसी नौजवान को सरे आम पीटते हुए उसकी पेशाब निकाल आने की गौरव-गाथा गाते वकील; गायब बच्चों को तलाशती माताएँ; सरेआम घरों, सड़कों, ट्रेनों में पीट-पीट कर मारे गए असहाय; धर्म के नाम पर मार-काट मचाते उन्मादी – कितने सारे परिंदे घायल पंख फड़फड़ाते होंगे!! नींद कैसे आती होगी?
बीमारी-तनाव के बीच नींद न आ पाना कितनी भयानक यातना है, रात कितनी अझेल हो जाती है; हम सब जानते हैं। शेक्सपीयर के मैकबेथ में मेमने जैसे भरोसे वाले राजा डंकन की हत्या कर रात भर न सो पाने वाली, (खून से सने समझ) हाथों को बार-बार धोती, हाथ में मोमबत्ती लिए रात भर घूमती लेडी मैकबेथ का चेहरा तो सत्ता और धन से दिपदिपाते लौहपुरुषों-चाणक्यों को भी डराता होगा!! किसी तरह नींद आ जाए – इसके लिए क्या जोड़-तोड़ करें, किसे मारें, किसे ‘विलेन’ बनाने वाली कहानी गढ़ें, किसे देशद्रोही करार करें, कैसे ‘विच हंटिंग’ में गरीबी-बेरोजगारी के मुद्दे भटकाएँ – बस नींद तो आ जाए! पर यहाँ तो शायद उल्टा हो जाता है – जितनी ‘विच हंटिंग’ करेंगे, वर्तमान मुद्दों को बरगलाते हुए जितना महान ‘भूत’ काल का गौरव-गान करेंगे –पीछे की ओर मुंह वाले उतने ही भूत, उल्टे पाँवों वाली उतनी ही चुड़ैलें नींद और आँखों के बीच आ जाएंगी। थोड़ा वक्त तो अपने ही शीशे में ‘निजी चेहरे’ के निशानों से रू-बरू होना पड़ेगा; पूरे चौबीस घंटे तो महान ‘सार्वजनिक चेहरा’ मदद नहीं करेगा।
खैर, ये भावुक बातें हैं। लिहाज में ऐसे लेख आते रहेंगे तो ‘राग दिल्ली’ कैसे चलेगा? इसलिए जिस घटना ने नहीं लिख पाने की वर्तमान जड़ता तोड़ी, उसका जिक्र करें।
कुछ दिन पहले खबर पढ़ी कि 1985 में दिल्ली में हुए ट्रांजिस्टर बम विस्फोटों के सिलसिले में जिन 59 लोगों को अभियुक्त मान कर पकड़ लिया गया था, उनमें से (अब तक जीवित!) 30 लोगों को अब आरोपमुक्त मान कर छोड़ दिया गया है।( ये बर्बर, कुरूप कांड, दिल्ली में 1984 के दंगों के घटनाक्रम के बाद हुआ था। ज़हर से तो ज़हर ही फैलता है। ) अदालत के फैसले में इन मामलों में जांच को ‘दोषपूर्ण, अन्यायपूर्ण और अनियमितताओं तथा तमाम कमियों से भरी’ पाया गया। ( शब्दशः अनुवाद नहीं) इन 59 में 19 इस लंबे दौर में, बिना न्याय की ‘क्लीन चिट’ पाए, अपराधी-आतंकवादी होने के कलंक के साथ ही मर गए।
अदालत ने अब पुलिस की अविश्वसनीयता और प्रताड़ित करने वाले तौर-तरीकों के लिए खिंचाई की है। इसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है – कितनी बेशर्म-गाथाएँ गाएँ। बस, कभी-कभी ( हमेशा नहीं) लगता है कि अदालतें भी हैं, देर-सबेर न्याय भी है। इस मामले के एक ही और धिक्कार-प्रसंग का जिक्र कर दें कि (अब घोषित जिंदा-मर चुके निरपराधियों के) ‘अपराध’ भी, 21 साल बाद, सितंबर 2006 में ‘तय’ हुए जबकि साधारणत: एफ़आईआर होने के तीन महीने के भीतर होने चाहिए थे। फिर इस मामले में दिल्ली पुलिस की ‘ओरिजिनल’ एफ़आईआर ‘खो’ गई थी। तो ये है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जिसके भरोसे हमें दंगाइयों को सख्त से सख्त सज़ा देने के आश्वासन दिये जाते हैं।
खैर! ये सब मामूली परिवारों के ‘अपराधी’ तो फिर भी भाग्यवान रहे कि इनको (अपने देश में अब उन्मादी भीड़ों और अर्धशिक्षित, खास तौर से हिन्दी-भाषाई मीडिया ने, गरीब, व्यवस्था-विरोधियों के मामलों में ‘अभियुक्त’ और ‘अपराधी’ का अंतर, खतरनाक तरीके से मिटा दिया है) को सबक सिखाने के लिए अदालतों पर देश (यानी भीड़) की ‘सामूहिक चेतना’ यानि ‘कलेक्टिव कोनसिएंस’ हावी नहीं हुई, जो इस ‘व्हाट्स एप’ जागृत, देशभक्त काल में बड़ी से बड़ी अदालतों तक पर हावी हो जाता है। फेसबुक पर मर्दवादी वीरों ने ‘ अगले चौराहे पर फांसी दो’ की गर्जना नहीं की। इन्हें मृत्युदंड नहीं मिला – नहीं तो आज, फैसले के बाद भी, न्याय शर्मिंदा-नंगा होकर सिर नीचे किए खड़ा होता। आखिर हम मार ही तो सकते हैं, गलत तरीके से किसी को मार कर फिर उसे जीवन दे सकें, उससे माफी मांग सकें, इतने समर्थ तो हुए नहीं।
अपराध की सजा तो ज़रूर होनी चाहिए, पर सही तरीकों और सही समय से प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए ताकि न्याय शर्मिंदा न हो। पर एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जब ‘अभियुक्त’ ( असली या ‘गढ़ा गया’) अगर गरीब-मजलूम हो हमारी, (खासकर अंदर से नपुंसक पर शब्दों में ‘मर्दाना’ मध्यवर्ग की, कुछ नैतिक न कर पाने की कायर हताशा से उपजी) लात मारने की इच्छा प्रबल हो जाती है। गरीब-मजलूम को लात मारना सुरक्षित होता है, कायर-कुंठित मन को नैतिक दिलासा भी मिलता है। अगर हम जाने-अनजाने इस मध्यवर्ग जैसे हैं, तो ऐसे प्रसंगों का ‘पारायण’ करें, खुद को सुधारें, ‘अंतरात्मा’ को कुरूप होने से बचाएं – वरना किसी दिन ‘लेडी मेकबेथ’ जैसी नींद न आने और अंधेरे-अकेलेपन में खून सने हाथ धोने की अभागी बीमारी हमें भी लग सकती है। इसलिए, दूसरों को समझाने के लिए कुतर्क न करें, अपनी अकेली उनींदी रातों की चिंता करें।
गरीब-पीड़ित को न्याय दिलाने में (बल्कि, उनके साथ अन्याय न हो जाए), ऐसी संवेदना रखने का संदेश देते हुए, पिछले दिनों दिल्ली से चंडीगढ़ हाई कोर्ट तबादले पर गए चर्चित न्यायमूर्ति मुरलीधर (उन पर न्यायमूर्ति टाइटिल कितना अच्छा लगता है!) ने अपने विदाई भाषण में, अंधेरे में दीपशिखा जैसी कुछ बातें कीं। न्याय में ‘न्यूट्रेलिटी’ ( बंजर ‘उदासीनता’ नहीं, संवेदनशील-सक्रिय ‘निष्पक्षता’) की व्याख्या करते हुए उन्होने कहा कि न्यायाधीश को “ न्याय प्राप्त कर सकने की क्षमता ( यानि ‘हैसियत’, बल्कि दो टूक कहें तो ‘औकात’) को आँकते हुए, ( न्याय मांगने वाले ) कमजोर और समर्थ-ताकतवर प्रार्थी में फर्क करने की समझ भी होनी चाहिए और कमजोर की तरफ झुकाव रखना चाहिए, ताकि न्याय के दोनों पलड़े बराबर रह सकें और दोनों पक्षों के बीच न्याय प्राप्ति में बराबरी हो सके।“
सुनहरे-समझदार शब्द!! न्यायमूर्ति मुरलीधर ने इसी सिलसिले में ‘गांधीजी के मशहूर जंतर’ का भी जिक्र किया कि अगर कभी फैसला लेने में संशय हो तो सबसे गरीब-हताश, मजलूम का चेहरा याद करो और सोचो कि जो काम करने जा रहे हो, जो फैसला ले रहे हो, उससे उस गरीब का भला होगा, उसके आँसू पुछेंगे। इससे तुम्हें सही राह मिलेगी और अहंकार भी पिघलेगा।
तो मित्रों! चाहे आपको अपने सार्वजनिक जीवन में चेहरे पर देश-जाति के लिए बलिदानी आंसुओं की कितनी भी परतें चढ़ानी पढ़ें, चाहे कितने भी तरीकों के उन्मादों के नालों में आम जन की बेहतरी के मुद्दे बहा देने पढ़ें – पर फिर भी अकेले अँधेरों में नींद न आने की डरावनी तकलीक झेलनी पड़े – तो गांधी जी का ये जंतर हर हाल में रामबाण औषधि है, सच्चे मन और सच्चे तरीके से अपना कर तो देखें।
क्योंकि, बावजूद हज़ार मतभेदों के हम ‘जनता’ की तो यही शुभकामना रहेगी ना, कि आप – जो हमारे नेता हैं- आपको खूब अच्छी नींद आए- ऐसी नींद जो किसी छल-तिकड़म से नहीं, बस, मन की निर्मलता से आती है। और आप भी जानते ही होंगे कि अकेले अंधेरे में, खुद से झूठ न बोल पाने की असहायता के बीच, पंख-नुंचे बेबस परिंदों की भुतहा लगती फड़फड़ाहट के बीच, नींद न आना कितनी बड़ी यातना है। आप को यह यातना न झेलनी पड़े, तभी तो आप स्वस्थ-निर्दोष नींद के बाद राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। आप-हम, हिन्दू-मुसलमान- सिख-ईसाई, इस देश के – बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को निश्चिंत-निर्दोष नींद का अमृत मिलता रहे, यही शुभकामना है।
लंबे समय तक सम्पादन और जन-संचार से जुड़े रहे राजेन्द्र भट्ट अब स्वतंत्र लेखन करते हैं।
हिन्दी वैब पत्रिका ‘ राग दिल्ली ‘ से साभार