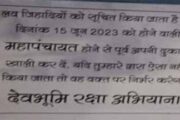चन्द्रशेखर तिवारी
हाल ही के वर्षो में ’बाटुइ’ शीर्षक से प्रकाशित कविता संग्रह कुमांउनी साहित्य में रुचि रखने वालों लोगों के लिए एक नायाब कृति के रुप में उभर कर आई है। वरिष्ठ रचनाकार ज्ञान पंत द्वारा इस संग्रह में 258 लघु कविताएं तथा 35 बड़ी कविताएं शामिल की गई हैं। जापान की हाइकू विधा की तर्ज पर बुनी गयी इन छोटी-छोटी कविताओं को कवि ने कुमाउंनी बोली में ’कणिक’ की संज्ञा प्रदान की है । कणिक का शाब्दिक अर्थ है छोटे – छोटे महीन कण । सीमित शब्दों में होने के बाद भी अन्ततः यह कविताएं पाठकों तक अपनी बात रखने में पूरी तरह सक्षम दिखाई देती हैं। पुस्तक का शीर्षक है ‘बाटुई , ‘ ’बाटुइ’ यानि हिचकी आना अर्थात अपनों की फाम (याद) करना। पहाड़ में व्याप्त धारणा के मुताबिक जब किसी व्यक्ति को ’बाटुइ’ लगने लगती है तो समझा जाता है कि उसका प्रियजन उसे बेपनाह याद कर रहा है। यही बात ज्ञान पंत जी की इन कविताओं में भी लागू होती हैं जो एक तरह से अपने प्रिय पहाड़ को बाटुई लगाती हुई प्रतीत होती हैं।
लखनऊ प्रवासी ज्ञान पंत को यदि चलते-फिरते पहाड़ की संज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। खुद के कन्धे में पहाड़ की गठरी लादे आप उन्हें कहीं भी देख सकते हैं। कवि सम्मेलन हो या रामलीला व होली के आयोजन हों अथवा प्रवासी संस्थाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम, आकाशवाणी से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर उनकी उपस्थिति बराबर बनी रहती है। मौका मिलते ही जहां उनकी यह गठरी खुली नहीं कि बस छोटी-बड़ी व रंग-बिरंगी पुन्तरियों में दुबका पहाड़ बाहर को फटक मारने लग जाता है। एक-एक कर समूचे पहाड़ के दृश्य सिनेमा की रील की तरह आंखों के सामने जीवंत होने लगते हैं। क्या जो नहीं समाया रहता इनकी पुन्तरियों में…..!! सभी कुछ तो है धुर-जंगल में दहकते लाल बुरांश की दमक…पेड़ों में बासती घुघुती-न्यौली की विरह वेदना…रोपाई के दौरान खेतों में लगने वाले हुड़किया बौल के गीत हर्याव के तिनड़ों व बग्वाली के च्यूड़ों की आशीष…..सांझ होते ही अपने गोठ को सरपट दौड़ लगाती बिनुली चम्फुली..,गाड़-गध्यार से आती सुसाट-भुसाट….नौल्-धारों का मीठा पानी, म्याल-कौतिक में हुड़के की गमक में भाग लगाते गीत….चैत माह में घर-घर ऋतुरैण गाते कलावन्त….गांव की पगडंडियों की तरफ नजर अटकाई बैठी कई बूढ़ी आखें…..शाम के झुरमुट में हरु, छुरमल व देवी के थान पर जलती दीये की बाती और टुन-टुन बजती घण्टियों का स्वर….और वीरान पड़ी बाखलियों की पीड़ा व आंगन के किनारे खड़े दाड़िम-माल्टा के पेड़ों पर पसरा अकेेलापन…आदि-आदि…इन पुन्तरियों में परदेश बसे उस पहाड़ी समाज़ की वह पीड़ा भी समाई हुई है जिसके कारण उसे अपनी जड़ों से अलग होना पड़ा। सीमान्त जनपद पिथौरागढ में बेरीनाग के समीप बसा कवि का पुश्तैनी गांव गरांऊ , लखनऊ में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लुकाछिपी के इस खेल में कभी पहाड़ आगे तो कभी कवि पहाड़ के पीछे आ जाता है। रचनाधर्मिता के इसी उपक्रम में कवि अपने बचपन की अनमोल यादों किस्से-कहानियों के सहारे पहाड़ के साथ खुद को भी जीवंत बनाये रखने में हरदम सफल सिद्ध हुआ है। यही वजह है कि पंत जी की हर रचना सुधी पाठक वर्ग को पहाड़ की बाटुइ लगाकर उसे आत्मसात कर जानने व समझने को उद्यत करती रहती हैं।
हांलाकि ज्ञान पंत के ईजा-बाबू कई सालों पूर्व अपने पुश्तैनी गांव गरांऊ को छोड़कर लखनऊ में आ बसे थे और ज्ञान पंत का जन्म भी यहीं हुआ,पढ़ाई-लिखाई, नौकरी व रहना-सहना सब यहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद भी उनका ठेठ पहाड़ी अन्दाज उन्हें किसी भी तरह लखनऊवा नहीं होने देता। घर वालों से अपनी दुदबोली कुमांउनी में होने वाली बातचीत, गरमी की छुट्टियों के दौरान गांव में बिताये पलों और सौगात के रुप में आमा-बड़बाज्यू से प्राप्त अनगिनत किस्से कहानियों ने ज्ञान पंत को पूरी तरह पहाड़ी बना दिया। बचपन से ही पहाड़ का भूगोल वहां का जनजीवन व उसकी आन्तरिक वेदना उनसे जुड़ी रही और इस तरह पहाड ज्ञान पंत के रग-रग में बस गया। बाद में कुमाउनी साहित्य लेखन की तरफ धकेलने में आकाशवाणी वाले बंशीधर पाठक ‘जिज्ञासु’ जी की प्रेरणा ज्ञान पंत के लिए अतयंत सहायक सिद्ध हुई। आवास-विकास परिषद् की नौकरी में रहते हुए छुट-पुट तौर पर लिखते रहे और सेवानिवृति के बाद लिखने का यह क्रम अब नियमित होने लगा है। इधर कुछ सालों से ज्ञान पंत सोशल मीडिया में भी ’बैठे ठाले’शीर्षक से वे गांव घर से जुड़े रोचक किस्सों को श्रंखला के रुप में सामने लाने का भी काम कर रहे हैं। पहाड़ी जन जीवन के प्रति उनका गहरा मोह ही दरअसल उनकी रचनाधर्मिता को जीवन्त बनाए हुए है।
ज्ञान पंत की कविताओं में पूरा पहाड़ बसा हुआ दिखता है। उनकी कविताएं मौजूदा सामाजिक व सांस्कृतिक सौन्दर्य का बोध कराने के साथ ही साथ खालीे हो रहे पहाड़ की पीड़ा को भी सहज रुप से प्रस्फुटित करती हैं। आज पहाड़ के गांव जिस तरह से खाली हो रहे हैं उस पर कवि की चिन्ता जायज है। गांव को हमने छोड़ दिया अब जिसे अब लंगूर-बन्दरों ने कब्जा लिया… न जाने किसकी नजर लगी पहाड़ को कि घर,गांव व गधेरे सब बंजर से हो गये… अपने ही गांव में अब मैं मेहमान सा हो गया…हमारे रहने तक ही पहाड़ है फिर कोई नहीं रहेगा पूछने वाला…बेहद मार्मिक भाव में कवि की कुछ कणिकाएं पहाड़ के वर्तमान को कुछ इस अंदाज से देखने का यत्न करती हैं-
हमैलि गौं छाड़ि दे
गुणि बानरैलि कब्जै ल्है!
पत्त नै कै नजर लागी पहाड़ कै
घर, गौं, गाड़ सब बांज् पड़ि गईं!
अपुण गौं में पौण भयूं!
हमन छन् जाणै पहाड़ भै
फिर क्वे पुछनेर न्हां!
पहाड़ में गौं-बाखलियों की नराई लग जाने से कवि का संवेदनशील मन एकाएक जाग गया है। वह लखनऊ से अपने गांव गराऊं पहुंच जाता है। वहां उसे बन्द दरवाजों के सांकल पर ताले लटके दिखते हैं रोजगार, पानी, इस्कूल-कालेज, अस्पताल, दवा-डाॅक्टर जैसी तमाम अन्य सुविधाओं की कमी और सुख-सुविधाओं की बढ़ती चाहत से पहाड़ मैदान में बसने को आतुर होने के दृश्य विचलित कर देते हैं। गांव के बूढ़े-सयानों पीड़ा आहत करने लगती हैं। ऐसे में वह गौं-बाखलियों के माध्यम से प्रवास में बस गये लोगों को पहाड़ आने का आत्मीय अनुरोध करता है कि मेरे पोथिलो एक बार किसी तरह पहाड़ आ ही जाओ यह वीरान बाखलियां तुम्हारा राह ताक रही हैं।
पोथी ! ऐ जाने त कस हुन
बोट फयि रौ,माल्टा झुकि पड़ि रौ
चाड़-प्वाथ ऊंण रयीं,तु लै ऐ जानैं धैं
गुन्याव में दम्मू-नगांर बाजन तेरि याद में
छो फुटन इजरकूं नौव में
पांणि ऐ जान घट रिंगंन,गूल सुसाट पाड़ैनि
दिगौ! तू ऐ जानै त रौन छैं आ्ग है जान
छिलुक ल्ही बेर तकैं देखन्यूं इजू
मैं बाखयि छूँ कैकी इंतजारी में आजि लै ज्यून छूँ ।
अपनी घर-कुड़ी बेचकर मैदान बस गये कुछ लोग जब निजी फायदे के चलते कभी-कभार पहाड़ पहुँच जाते हैं तो कवि का अन्तर्मन कसमसा उठता है और वह उन्हें लानत देकर कहने लगता है कि पहाड़ आये तो हो पर यहां की हरी-भरी धरती को बंजर बना गये हो।
तुम ऐ गोछा पहाड….
लुछि-लाछि बेरि ल्हीनै गोछा
ढुंग पिर के नि छाड़ि,
बोट-डाव,गाड़,गध्यार,रौड़
सब खालि करि गोछा
तुम ऐ गोछा पहाड़….
द्याप्तनक नाम पर जागर लगै
बवाल फेड़ि गोछा
हरी-भरीं धरती कैं बाजिं पाड़ि गोछा
तुम ऐ गोछा पहाड़….
पुर्खनें जमीन त् जैजाद बेचि गोछा
चार डबलनां खतिर
आपणिं पच्छयाण ले मिटै गोछा
तुम ऐ गोछा पहाड़…!
ज्ञान पंत की कणिकाएं राजनीति व भ्रष्टाचार पर प्रहार करते समय अत्यंत तीक्ष्ण आक्रोश में नहीं रहतीं अपितु वह सामान्य तौर पर संयम बरतती हैं और सहजता के साथ अपनी बात को कह देने में सिद्धहस्त दिखती हैं। आम जन की पीड़ा उनकी कविताओं के हर शब्दों में साफ झलकती रहती है। सरल शब्दों में कहा जाय तो उनकी कविता और समाज में पसरी तथाकथित भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था के मध्य एक वैचारिक संघर्ष चलता रहता है। उनकी कविताएं हमेशा न्याय संगत व सही बात के पक्ष में खड़ी दिखती हैं।
राजीनति आपण जाग् भै
सही बात में त ’होय’ कयी कर।
इनैरि करतूत देखौ….
नेता ’छव’जा देखीनीं।
सबनां खपुन म्वाव
वाह रे नेता अहा रे चुनाव!
’लोक’ हरै रौ
तबै नेता ’तंत्र’ है रौ।
मौजूदा शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली से कहीं-कहीं पर कवि का मन बुरी तरह खिन्न भी हो उठा है। तभी तो व्यवस्था को चलाने वाले तथाकथित राजदारों पर वे बहुत करारा व्यंग्य करते हैं उनकी कल्पना में उस राज व्यवस्था के हालात इस कदर हो गये हैं कि वहां आम जन की फरियाद सुनने वाला कोई है नहीं है…. हो भी कैसे आखिर जहां ’बहौड़’ पटवारी बन गये हैं और ’ग्वाण’ सरकारी बाबू बन बैठे हैं और अनशन पर बैठी ’बकरियां’ हर रोज बलि का शिकार बन रही हैं…आदि-आदि। प्रस्तुत संग्रह में ’सरकार’ कविता में कवि कहता है।
बानरा राज में
गुणि मंत्री,बाघ संतरी
स्याव दफ्तरी,ग्वाण बाब् सैप
बहौड़ पटवारि,बल्द सटवारि
बाछ तहसीलदार,कुकुर लेखपाल और कुकुड़ चौकिदार
यसि में बकार् अनसन में पैठि रईं
बेई द्वि त आज चार कम है गईं
आब मोक्कदम चलौल
शिबौ च्योड़ी घुघुत के न्याय करौल !
लोकोक्ति परम्परा के तहत यह कणिकाएं आम जन तक अपने गूढ़ संदेशों को बहुत सहजता के साथ प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ दिखती हैं। समाज को सजग करती ’बाटुइ’ संग्रह की कविताओं का विशिष्ट अंदाज कुछ इस तरह दिखाई देता है।
मतलबै दुन्नी में ले
बेमतलब के नि भै।
अन्यार देखां डरलै त
दिन में ले उज्या्व नि हो।
गुम चोट में
ल्वे नि ऊंन।
घौल मैई रौले त
कसिक उड़लै।
कतुकै अगाश पुजि जा
खुट त भीं मैई धरलै।
सोच नि भई त
मनखी ‘बोनसाई’ है जां छ।
बाटुइ कविता संग्रह में ज्ञान पंत के आसपास पहाड़ इस कदर रच-बस गया है कि उसके दिलो दिमाग के में हर बखत यहां के तमाम दृश्य चित्र उतरते बनते रहते हैं। अनायास ही इन दृश्य चित्रों में कवि की कल्पना एक से बढ़कर एक बिम्ब उभरने लगते हैं जिनमें सुख के साथ दुःख के रंग भी हैं। पहाड़ के डाने-काने, अगास में घुमड़ते बादल,गाड़ गधेरों का सुसाट, खेतों में लहलहाती धान-गेहूँ की फसल के साथ दूसरी ओर रड़ते-बगते पहाड़ व धुर डानों में गिरते बज्र के भी मार्मिक चित्र हैं।
अगाश बणों, यमैं सूर्ज दिखौ
चमचमान जंगल बैणांये हरिया-हरी बोट लगायै
गाड़ गध्यार,रौड़ और ताल बैणांये
छीड़ दिखायै, पंचेश्वर ले होल् हां
जां सरयू,रामगंगा,गोरी, काली, पनार भेंटाल
और गौं देखियौल त्यर,म्योर या कैं को ले होल् त
के फर्क पणौ…मैस त सबै ठौर एकनस्से हुनेर भ्या
यतु हैयी बाद तु देखियै खेतन में ग्यंू धान पौयी जाल्
कपाव में हाथ लगै मलिकै चालै त
बादल दिखियाल औड़ाट-घौड़ाट ले होल
बिजुलि चमकैलि धुर-डानन में
कयीं बजर लै पड़ौल… तु झन घबरायै
पहाड़ में चैमासे शुरुआत यसीकै हुंछ
और तब दुन्नी हरिया हरी है जैं
अब तु पेंटिंग में ले भली कै देख सकछै
पहाड़ में जिन्दगी और जिन्दगी में ’पहाड’ ले।
हरफन मौला जनकवि गिरदा को कवि अपने आदर्श नायक के रुप में देखता है। उसका संवेदनशील मिजाज और जनगीत उसे हर पल बांधे रखता है। सम्भ्वतः इसीलिए कवि की कई रचनाएं गिरदा की रचना धारा के सापेक्ष चलती रहती हैं। प्रस्तुत ‘बाटुइ’ कविता संग्रह में भी ‘गिरदा’ पर आधारित कुछ कविताएं हैं जो सामाजिक आन्दोलनों के परिप्रेक्ष्य में गिरदा के गीतों को मुखरित करती हैं और जुल्म व शोषण के प्रति धात लगाती हुई लगती हैं।
गिर्दा मतलब छाव् हौ
घोल है भ्यार आ
फटक मार,धार में जा
ढुङ्ग घुर्यों,मनखिन जगौ
हड़की रयी कुकुरन् डरौ
लुकि रई स्यावन भजौ
और मैंस हुंणों सऊर सिखौ।
समाज के जन नायकों के महाप्रयाण के बाद उनकी यादों को महज रस्म-अदायगी तक सीमित करने की परम्परा को कवि ज्ञान कतई सही नहीं मानता। समाज पर तंज कसने को मजबूर यह कवि कह उठता है-
गिर्दा कैं मा्व पैराल
ए. सी. बिल्डिंग में
गीत-गोविंद गैई जा्ल
और फिर खै-पी बेरि
सब बम्-बजाल….
पहाड़ की नराई में आकण्ठ डूबे कवि को अपना पुश्तैनी गांव बार-बार याद आता है।
सुद्दै जि है रौ निस्वास लागण
त्वीलि फाम करी और बाटुइ लगैन्हेल
ढुङ्ग-पाथर है रईं जिन्दगी में
कभै कैले चार छिंट पाणिंक खिता त
सुखी पात जस कल्ज आफि है ताल है जांछ
ओर घटै चार दुन्नी रिंगंन भै जैं,
भागी कभतै तालुन ले लै ढुङ्ग खित दियी कर
मैं पांणिक छलबलाट आजि ले भल लागौं।
कुल मिलाकर ज्ञान पंत की कविताओं में पहाड़ के प्रति गहन संवेदना झलकती है। मुख्य बात यह है कि इनकी कविताएं मात्र नराई तक सीमित नहीं हैं अपितु वह पहाड़ के तमाम सरोकारों से भी जुड़ी हुई हैं। उनकी कविताओं में जहां पहाड़ के प्रति चिन्ता का भाव दिखाई देता हैं वहीं यह कविताएं पहाड़ को बचाने का आह्वान भी करती हैं। इस संग्रह के अभिमत में वरिष्ठ शिक्षाविद व भाषाविद् डाॅ. सुरेश पंत लिखते हैं कि ’ज्ञान पंत की कविता से गुजरना आज के समय ओस पड़ी दूब पर नंगे पांव गुजरना है……जो रोमांचित भी करती है,सतर्क करती है,ठंडक भी पहुंचाती है और कभी मीठी चुभन से अपने होने का अहसास भी…’। वहीं वरिष्ठ पत्रकार व कथाकार नवीन जोशी का कहना है कि इस संग्रह में शामिल ज्ञान पंत की कविताएं पहाड़ की बात करतीं हैं, परदेश गये युवाओं को धाद लगाकर आह्वान करती हैं कि सीधे रास्ते में आते रहो…इधर-उधर भटकना नहीं।
इस संग्रह में कई जगहों पर कुमाउनी दुदबोली के अनेक मोहिल शब्द भी आये हैं। इन शब्दों में गंगोली व कमस्यार इलाके की खास ठसक व मिठास भरी हुई है। निश्चित तौर पर यह तमाम शब्द कुमाऊं की शब्द सम्पदा को समृद्ध करने में अपनी महति भूमिका निभा रहे हैं। संग्रह में आये कुछ खास शब्द इस तरह हैं- जुन्यालि, उज्याव, दिगौलालि, बण्याट, कुथव, रनकार, निगरगण्ड, अतराट, कर्याड़ि, इजर, हवभान, आगहान, फट्याव, मनखियोव, ट्यो, फटक, पौण, गिजूण, गुईया-गुई, धनपुतई ,म्वाव, बम बजाल, खुटकूंण, क्याप, खबीस, सुसाट, दुबज्यौड़, मनसुप आदि।
निष्कर्ष रुप में इस संग्रह में शामिल कविताएं बिना लागलपेट के अपनी बात सरलता के साथ कहने में समर्थ हैं। अपनी कुमाउनी बोली-भाषा में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए यह ’बाटुइ’ कविता संग्रह खास साबित होगी ऐसी आशा है। इन कविताओं के मूल में निहित प्रेरणा पहाड़ के प्रति हमारी संवेदनशीलता को हमेशा बनाये रखे इसी कामना के साथ कवि ज्ञान पंत को इस संग्रह के प्रकाशन की कोटिशः बधाई व शुभकामनाएं।
पुस्तक: बाटुइ
रचनाकार: ज्ञान पंत
पृष्ठ: 112
प्रकाशन वर्ष: 2019
मूल्य: रु.100/-
प्रकाशक: पर्वतीय महापरिषद्,गोमतीनगर,लखनऊ
-चन्द्रशेखर तिवारी
दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र, देहरादून
मोबाइल: 8979098190