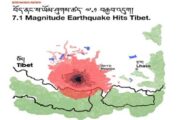दीपिका
11वीं, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल
‘जूठन’ सोने के बर्तन में भी कोई तवज्जों नहीं पा पाती। अजीब विडंबना है, यह जूठन सिर्फ अवशिष्ट खाना नहीं बल्कि हयात भी हो सकती है। ऐसी हयात जिसको हीन दृष्टि के तीर छलनी कर देते हैं। दुनिया की इल्मी जंग में बिना इल्म के कुचल दी जाती है। ऐसी ही एक हयात की जिंदगानी का अफ़साना है ‘जूठन’।
‘जूठन’ ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। आज हिंदी दलित साहित्य में जूठन का स्थान अद्वितीय है। यह उन मार्मिक व खुशनुमा लम्हों का संग्रह है जिन्हें लेखक ने अपने जीवनकाल में भोगा। इस मास्टरपीस की रचना हालाकि लेखक के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। इस बारे में लेखक कहते हैं – ” जूठन लिखना मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था ! ” यह पंक्ति पढ़ना, बिन पानी तड़पती मछली को देखने जैसा है। बस फर्क इतना है कि मछली अपने दर्द का बयां नहीं कर सकती लेकिन वाल्मीकि की तड़प ‘जूठन’ बन कर अमर हो गयी।
यह तड़प लेखक की ज़िंदगी में खाद-पानी की तरह थी। उनके जन्म से मृत्यु तक उनके अंदर की लौ में घी बनकर बरसती रही। जिस जाति से वह पैदाइशी ताल्लुक़ रखते थे, उन लोगों को ऊँची जाति वाले ‘चूहड़ा’ कहते थे। उन्होंने लिखा है – ” अस्पृश्यता का माहौल कि कुत्ते-बिल्ली, गाय-भैंस को छूना बुरा नहीं था लेकिन यदि चूहड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इनसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ काम की वस्तु थे। इस्तेमाल करो, दूर फेंको” ।
इसी मानसिकता का उदाहरण था ‘बेगार’ व्यवस्था का अस्तित्व। वे लोग तगाओं के घरों में सारा काम करते थे। इसके बावजूद उन्हें रात-बेरात बेगार करनी पड़ती। यानि ऐसी मजदूरी जिसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इसका एक कारण यह भी था कि वे लोग कर्ज़ में डूबे हुए थे। इसलिए किसी भी ज्यादती का विरोध नहीं कर पाते थे। पर कुछ समय बाद उन्होंने बेगार करने से इन्कार कर दिया। अंजाम यह हुआ कि – ” कुछ दिनों बाद दो सिपाही बस्ती में आए और जो सामने दिखा उसे बुला लिया। इलियास के बगीचे में बस्ती से पकड़ कर लाए गए लोगों को मुर्गा बनाकर पीटा जा रहा था। प्रत्येक प्रहार पर पिटनेवाला जोर से चीख उठता। खुले आम यह शौर्य-उत्सव मनाया जा रहा था। बस्ती की औरतें व बच्चे गली में खड़े दहाड़ें मार-मारकर रो रहे थे। ”
समाजशास्त्र में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट भी यही मानते हैं कि – ” सत्ता (स्टेट) सदैव हावी वर्ग की पक्षधर होती है। सारी व्यवस्था ही ऐसे बनाई जाती है जिससे कि यथास्थिति बरकरार रहे”। लेखक भी इस बात से इत्तफा़क़ रखते होंगे। वह लिखते हैं – लोकतंत्र की दुहाई देनेवाले सरकारी मशीनरी का उपयोग नसों में दौड़ते लहु को ठंडा करने के लिए करते हैं, जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं है। हज़ारों साल से इसी तरह दबाया गया कमजोर और बेबसों को।”
यह बेबसी न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। ‘अदम गोंडवी’ जी का एक बेहद खूबसूरत शेर है कि – ” इन्द्र-धनुष के पुल से गुज़र कर बस्ती तक आए हैं, जहाँ भूख की धूप सलोनी चंचल है बिन्दास भी है। ”
आर्थिक स्थिति के कारण दो जून की रोटी हासिल करना भी मुश्किल होता था। जठराग्नि बुझाने को – ” शादी-ब्याह के मौकों पर, जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहड़े दरवाज़ों के बाहर बड़े-बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा लेने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती। …. यह सब पाकर उनकी बाछें खिल जाती थीं। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी।” शायद इन्हीं घटनाओं के आधार पर राजेन्द्र यादव जी ने लेखक को इस कृति का शीर्षक ‘जूठन’ रखने का सुझाव दिया होगा।
जूठन के साथ-साथ सूअर भी उनके खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा था। सूअर केवल खाने में नहीं बल्कि पूजा-पाठ और व्यापार में भी काम आते थे। तगाओं के यहाँ भी पूजा में सूअर की बली दी जाती थी। एक पूजा के लिए लेखक को एक सूअर का बच्चा न चाहते हुए भी खुद ले जाना पड़ा। यह काम उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। मंदिर पहुँचने पर – ” उस व्यक्ति ने मुझसे कहा – लो छुरी और करो शुरू… माता का नाम लेकर। मेरे लिए यह क्षण किसी भयानक विस्फोट से कम नहीं था। … मैंने काँपते हाथों से छूरी उसके सीने पर रखकर दबाई। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा ‘और घुसाओ’ लेकिन छूरी आगे नहीं बढ़ रही थी। उस व्यक्ति ने छूरी की मूठ पर दबाव बढ़ा दिया था अपने हाथ से। लहु का फव्वारा फूटने लगा। लहु से मेरे कपड़े, हाथ, मुंह भीग गए थे।…बच्चा अभी भी चीख रहा था। छूरी उसके दिल को छेद चुकी थी लेकिन वह मरा नहीं था। जब काफी देर तक उसके प्राण नहीं निकले तो उन लोगों ने उसे धधकती आग में रख दिया। आँच लगते ही वह बच्चा चीख पड़ा। अचानक मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ।” यह ‘जूठन’ के सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। लेखक ने जिस तरह इन घटनाओं को शब्दों में बयां किया है, वह कृति को हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि बनाने की नींव है।
लेखक को इस मुक़ाम पर पहुँचाने की नींव उनके माँ-पिताजी का साहस और सहयोग थे। उस समय आज़ादी के आठ साल हो गए थे। स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खुलने लगे थे। लेकिन जनसामान्या की मानसिकता तो ज्यों की त्यों बेड़ियों में उलझी जंक खा रही थी। लेखक के लिए भी स्कूल जाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। वह लिखते हैं – तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊँ,और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊँ, जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार, स्कूल आना मेरी अनधिकार चेष्टा थी।”
‘स्कूल’ को भी समाजशास्त्री अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। फन्कशनलिस्ट शिक्षा को समाज में बाद की भूमिकाओं, या कार्यों के लिए छात्रों को तैयार करके समाज की जरूरतों को पूरा करने के साधन के रूप में देखते हैं। वहीं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट स्कूलों को वर्ग, नस्लीय-जातीय और लैंगिक असमानताओं को बनाए रखने के साधन के रूप में देखते हैं। लेखक के स्कूल में भी शिक्षक पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से खुद को आज़ाद नहीं कर पाए थे। एक बार हैडमास्टर ने ओमप्रकाश को पूरे स्कूल का झाड़ू लगाने का आदेश दिया। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ लेकिन उनके मन में तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊँगा। पर तीसरे दिन जब लेखक कक्षा में बैठ गया तो थोड़ी देर बाद अपनी मर्यादा भुलाकर हैडमास्टर ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ देते हुए चिल्लाने लगा। ” उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर काँपने लगा। हैडमास्टर ने लपककर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उँगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा के बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। … भयभीत होकर मैंने तीन दीन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सुखकर झरने लगे थे। … मेरा रोम-रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था “।
इन यातनाओं के साथ – साथ स्कूल ने लेखक को पुस्तकालय भी दिया। किसी ने कहा है न कि – ‘ जब आप एक अच्छी किताब खेलते हैं तो दुनिया में कहीं आपके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है ।’ लेखक के लिए दुनिया के दरवाजे भी इसी पुस्तकालय से खुले। वे बताते हैं कि – ” स्कूल में एक पुस्तकालय था , जिसमें पुस्तकें धूल खा रही थीं । इसी पुस्तकालय में पुस्तकों से परिचय हुआ था पहली बार । आठवीं कक्षा में पहुँचते – पहुँचते शरतचन्द्र, प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ डाला था। शरतचन्द्र के पात्रों ने मेरे बाल-मन को बहुत गहरे तक छुआ था । पढ़ने का एक सिलसिला आरम्भ हो गया था । उन दिनों मैं कुछ-कुछ अन्तर्मुखी हो रहा था। डिबिया ( ढिबरी ) की मन्द रोशनी में, माँ को उपन्यास , कहानियाँ पढ़कर सुनाने लगा था। न जाने कितनी बार शरतचन्द्र के पात्रों ने माँ – बेटे को एक साथ रुलाया था। बस, यहीं से शुरू हो गए साहित्य के संस्कार। अनपढ़ अछूत परिवार में जन्मे इस बेटे ने अपनी अनपढ़ माँ को ‘ आल्हा ‘ , ‘ रामायण ‘ महाभारत ‘ से लेकर ‘ सूर सागर ‘ , ‘ प्रेम सागर ‘ , ‘ सुख सागर ‘ , ‘ प्रेमचन्द की कहानियाँ ‘ , ‘ तोता – मैना के किस्से … जो भी मिला, सुना दिया’।
इंटर के अंतिम वर्ष में, लेखक को अहसास हुआ कि उन्हें जानबूझ कर प्रैक्टिकल करने से रोका जा रहा है। अंत में हुआ भी वही जिसका डर था, वह इंटर फेल हो गए। यह समय बहुत मुश्किल था उनके लिए। इसकी वजह से देहरादून में भी दाखिला लेने में काफी परेशानियाँ आईं। लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चयी होकर सभी परेशानियों का सामना किया। देहरादून में ही उन्होंने प्रतियोगिता पास कर ऑर्डेनेंस फैक्ट्री में ट्रेनिंग व काम करना शुरू कर दिया। यही आगे चलकर उनकी आजीविका का साधन भी बनी।
ओमप्रकाश को अब अपनी पत्नी चन्दा का भी अपने साथ ले जाना था। पर कोई भी उन्हें रहने को घर किराए में देने को तैयार नहीं था। यह उस समय के देहरादून की बात हैं जो फिर भी थोड़ा बहुत विकसित हो गया था। पर आडम्बर और पूर्वाग्रही मानसिकता का यह ‘विकास’ कुछ न कर सका। हर जगह उनसे उनकी जात पूछकर उन्हें घर देने से साफ मना कर दिया जाता। लेखक शुरुआत में ही कहते हैं कि – ” दलित – जीवन की पीड़ाएँ असहनीय और अनुभव – दग्ध हैं । ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके । एक ऐसी समाज – व्यवस्था में हमने साँसें ली हैं , जो बेहद क्रूर और अमानवीय है । दलितों के प्रति असंवेदनशील भी । ”
यह जाति सदैव उनके सर पर मंडराती रही। इसने उन्हें बेहद दर्द और यातनाएं तो दी पर एक संवेदनशील मनुष्य भी बनाया। एक ऐसा मनुष्य जो न सिर्फ अपनी जाति बल्कि महिलाओं व मजदूरों के हितों की माँग करने में हिचकिचाया नहीं। जब वह देहरादून में कार्यरत थे तो एक रात मूसलाधार बारिश के कारण मजदूर अपनी अस्थायी झोपड़ीयों में मलबा के तले दबकर मर गए। सुबह होने तक भी प्रशासन द्वारा जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इस कशमकश में लेखक ने एक कविता लिखी। जिसकी कुछ पंक्तियां कुछ इस तरह हैं –
” शब्द हो जाए जब गूंगे,
और भाषा भी हो जाए अपाहिज
समझ लो
कहीं किसी मजदूर का
लहू बहा है “।
उनका व्यावसायिक जीवन भी चुनौतियों से भरा पर सफल रहा। खासकर जब वह शिमला में कार्यरत थे। लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा। डॉक्टर कई टैस्ट के बाद भी उनकी बीमारी पहचान नहीं पा रहे थे। अंत: नोएडा में गंगाराम अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ। इस दौरान उनसे मिलने कई लोग आए। जिनमें से ज़्यादातर छात्र, लेखक व उनके पाठक थे। लेखक के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं रही होगी क्योंकि इससा कई गुना दुख वह पहले ही भोग चुके थे। उस दुख ने उन्हें संवेदनशील के साथ मजबूत भी बना दिया था। ऑपरेशन से पहले भी उनका कहना था – ” वैसे भी मुझे कभी भी मृत्यु का खौफ नहीं लगा । जब तक साँसें चल रही हैं तभी तक दुनिया भर की हाय – तौबा है । आँख बन्द होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है । यदि कुछ बचता है तो वह है आपके द्वारा किया गया काम अन्यथा कोई किसी को याद नहीं करता । न जाने किस क्षण में मेरे मन में मरने का खौफ खत्म हो गया था । अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी मैं अपने आपको सहज महसूस कर रहा था । ”
‘जूठन’ ने मानो प्याज़ रूपी समाज की एक-एक परत नोंचकर सामने रख दी। शायद यही वजह थी कि मैं अपनी समाजशास्त्र की पुस्तक द्वारा दिए गए चश्मे से इसे और बेहतर समझ पा रही थी। समाज का स्तर-विन्यास, सामाजिक व्यवस्था और जातिवादी सोच का निम्न स्तर सब सजीव हो उठा। वाल्मीकि भी धीरे-धीरे यह सब समझने लगे थे। यही कारण था कि उनके मन में इस व्यवस्था के प्रति अगण्य क्रोध व नफरत भर गई थी। लेकिन वह अंत में कहते हैं –
” आज सोचता हूँ इस त्रासद घड़ी ने जहाँ मुझसे बहुत – कुछ छीना है , वहीं मुझे बहुत कुछ ऐसा भी दे दिया है , जिसने मेरे भीतर जीने की एक गहरी ललक पैदा कर दी है । एक बहुत बड़े परिवार से मुझे जोड़ दिया है , जहाँ न जाति की दीवारें हैं , न धर्म की ।”
किताब की पंक्तियों में पीड़ा, क्रोध, सुख और आक्रोश साफ-साफ महसूस होते हैं। इन्हीं तत्वों ने तो इस शब्दों की रचना को एक वर्ग की आप-बीती का आइना बना दिया। अपने व्यावसायिक व साहित्यिक जीवन में इतनी सफलता पाने पर भी वह कहते हैं – ” उपलब्धियों की तराजू पर यदि मेरी इस व्यथा-कथा को रखकर तौलोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा।” यही उदारता और सादगी तो है जिसने इस हयात के अफसानों को ‘जूठन’ बना दिया।