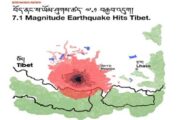हरीश चंद्र अंडोला
वन्यजीव-मानव संघर्ष में पहाड़ के आंसू बह रहे हैं। वहीं, ‘लिविंग विद लेपर्ड’ प्लान धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। जबकि महाराष्ट्र की तर्ज पर गढ़वाल मंडल के गुलदार प्रभावित कुछ जिलों व गांवों में आजमाए जा रहे इस प्लान के सुखद परिणाम मिले हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व नैनीताल में जनहानि रोकने को रैपिड रिस्पांस टीम का गठन तो दूर, इस प्लान पर अमल तक नहीं किया जा सका है। महाराष्टï्र के हिंसक वन्यजीव गुलदार प्रभावित जुनर गांव में इस फार्मूले को अपनाया गया था। इसके बेहतर परिणाम सामने आने पर 2017 में उत्तराखंड में भी इसे आजमाने की तैयारी की गई। गढ़वाल मंडल के टिहरी, पौखाल व अगरोड़ा में तो 2016 से इस पर काम चल रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के दिशा निर्देशन में पौड़ी आदि तमाम क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा। वहां भी टकराव को कम करने में मदद मिली है। मगर कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के बावजूद इसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। हालांकि प्रभागीय वनाधिकारी की अगुआई में लिव विद लेपर्ड फार्मूले पर फाइल तेजी से आगे बढ़ी भी है। हम जितना ज्यादा जंगल के नज़दीक पहुंच रहे हैं ये समस्या उतनी ही अधिक बढ़ रही है। मध्य हिमालयी जंगल में भोजन की कमी की समस्या भी बनी हुई है। जिसके चलते गुलदार जैसे जानवर भोजन के लिए रिहायशी बस्तियों की ओर आ रहे हैं। जंगल में हिरन-कांकड़, जंगली मुर्गे जैसी जीवों की तादाद घटी है।राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक कहते हैं इस संघर्ष के बढ़ने के पीछे कचरा प्रबंधन न होना एक बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है। जंगल के पास कचरा फेंका जाता है। जहां जानवरों को आसानी से भोजन मिल जाता है। गुलदार ही नहीं हरिद्वार में हाथी जैसे जानवर भी आसान भोजन के लिए कचरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं।वन्यजीवों के पारंपरिक कॉरीडोर खत्म होना भी वन्यजीवों की आवाजाही को बाधित कर रहा है और उन्हें रिहायशी इलाकों से गुजरने पर मजबूर कर रहा है। वन क्षेत्रों में बिना सावधानी के बनायी गई सड़कें, नहर वन्यजीवों के रास्ते में आ रहे हैं।उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरह अन्य वन्यजीवों की स्थिति के आंकलन की कोशिश नहीं की गई। वन विभाग को ये अनुमान तक नहीं है कि राज्य में कितनी संख्या में गुलदार होंगे। शिकारी जॉन हुकिल का अनुमान है कि राज्य में 6-7 हज़ार तक की तादाद में गुलदार हो सकते हैं। तो समस्या कितनी बड़ी है, गुलदार क्यों रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। न कि कोई घटना हो जाने के बाद उस पर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई।इसके साथ ही जंगल से लकड़ी, घास, चारे के इंतज़ाम के लिए लोग जाते हैं। बहुत से मामले ऐसे हैं जब जंगल के अंदर जानवर का हमला हुआ है। यहां लोगों को भी जागरुक किए जाने की जरूरत है। राज्य में जंगली जानवरों के बढ़ने के साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ी है। मानव वन्यजीव संघर्ष उत्तराखंड से पलायन की वजहों में भी शामिल है। विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर बहुत अधिक नहीं दिख रहा। इसलिए जानवरों को भी इंसानों के गुस्से का खामियाज़ा उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत होती है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग के लोग समय पर नहीं पहुंचते। खुद वन विभाग में फील्ड
ड्यूटी कर रहे कर्मियों के पास जंगल में कॉम्बिंग के दौरान जरूरी रक्षा सामाग्री नहीं होती संसाधनों और स्टाफ की कमी के चलते उत्तराखंड वन विभाग जंगल के नज़दीक रहने वाले लोगों का दोस्त नहीं बन पा रहा। वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम हिंसक वन्यजीव प्रभावित गांवों पर नजर रखेगी। ग्रामीणों को जंगल या वनक्षेत्रों से सटे खेतों में कैसे, कितने बजे तक जाना है यह भी बताया जाएगा। साथ ही शौचालय, आंगन व गलीनुमा गांव के रास्तों पर सौर ऊर्जा या बिजली जलाने को जागरूक किया जाना है। गुलदार प्रभावित पर्वतीय जिलों में साल 2018 में वर्ष 2012 जैसे हालात पैदा हुए थे। तब अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत व पिथौरागढ़ में 12 लोग गुलदार का शिकार बने थे। 70 घायल भी हुए। 2020 में आंकड़ा बढ़ गया। 15 लोग मारे गए और 76 घायल हुए। जवाब में 40 गुलदारों को नरभक्षी होने की कीमत भी चुकानी पड़ी। राज्य गठन से अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो संघर्ष में 91 इंसान व 155 गुलदार ने अपनी जान गंवाई।डीएफओ ने बताया कि लिव विद लेपर्ड प्लान पर प्रयास तेज किए गए हैं।ú
पेड़-पौधे और वन्य जीव अगर वोटर होते तो राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में उत्तराखंड में हर साल धधकने वाली वनाग्नि की समस्या के समाधान के लिए जरूर कोई न कोई वादा होता। वनों में लगने वाली आग को रोकने की रणनीति या कार्यक्रम सीधे-सीधे मतदाताओं को नहीं रिझाते, इसलिए राजनीतिक दलों का ध्यान फायर सीजन में ही चुनाव होने के बावजूद इस पर नहीं गया। 71 प्रतिशत वन भूभाग वाले प्रदेश के राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त हैं और जिम्मेदार विभाग गरजते-बरसते मौसम के भक्त हुए जा रहे हैं। इस वर्ष जनवरी-फरवरी माह में उत्तराखंड में करीब 50 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी है, पहाड़ों की जमीन में नमी समाई है और चाल-खाल में भी आगे तक पानी रहने वाला है।राज्य में हर साल औसतन 1,978 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से सुलगता है। इससे वनस्पति एवं जैविक संपदा का नुकसान तो होता ही है, हिमालयी क्षेत्र का पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है। पिछले 12 वर्षों में उत्तराखंड के जंगलों में आग की 13,574 घटनाएं हुई हैं, फिर भी आग बुझाने की विभागीय तकनीकी पारंपरिक ही है। पिछले तीन-चार वर्षों से वनाग्नि की सूचना प्रसार के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाने लगा है। आवश्यकता तो नई तकनीकी के इस्तेमाल के साथ जवाबदेह व्यवस्था विकसित करने की है। इसी कमी के कारण घटिया इरादों के लिए जंगलों में आग लगाने वालों को दंडित किए जाने के उदाहरण कम मिलते हैं और वन अपराधी निडर हो कर यह सब करते रहते हैं।यह यहां की प्रकृति की देन है कि जंगलों में लगने वाली आग सतह पर ही फैलती है जिससे पेड़ों को कम नुकसान होता है, लेकिन छोटे पौधों एवं बहुमूल्य वनस्पतियों को इससे काफी हानि होती है। यह जंगलों में पनपने वाली जैवविविधता के लिए भी बड़ा खतरा है। जंगल में आग के दो कारण हैं। पहला मानवजनित है तो दूसरा प्राकृतिक। मानवजनित कारण भी दो तरह के हैं। छोटी-छोटी लापरवाही वन संपदा के लिए घातक हो जाती है। बीड़ी-सिगरेट या घरों के आस-पास झाड़ियों में लगाई गई आग को बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं और यही आग अक्सर पूरे जंगल को सुलगा देती है। मानवजनित कारणों में कुछ असामाजिक तत्व अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए इरादतन आग लगा देते हैं। कभी जंगली जानवरों के शिकार के लिए तो कभी आग के बाद उगने वाली हरी-घनी घास के लिए यह खतरनाक खेल खेलते हैं। कई बार वन विभाग के ही काले भेड़िये अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए भी रक्षक से भक्षक बन जाते हैं। इस आग से हवाई पौधारोपण एवं अवैध कटान पर भी पर्दा पड़ जाता है। यह स्पष्ट है कि वनों की आग का मुख्य कारण मानव ही है।कुछ मामलों में प्राकृतिक रूप से भी जंगलों में आग लग जाती है। जानवरों की आवाजाही से ऊंचे पहाड़ों से पत्थर लुढ़कते हैं, जो कई बार टकराहट में चिंगारी छोड़ जाते हैं। यह चिंगारी जब सूखी घास एवं पत्तियों के संपर्क में आती है तो जंगल में आग की घातक कहानी लिख जाती है। जंगलों की आग के लिए काफी हद तक चीड़ के पेड़ भी जिम्मेदार हैं। इनकी सूखी पत्तियां गर्मियों में जंगलों में आग फैलाने में पेट्रोल सरीखा काम करती हैं। साथ ही ये बारिश के पानी को जमीन में रिसने से रोकती हैं। चीड़ के जंगलों में कोई और पौध नहीं पनप सकती है। चीड़ की यह असहिष्णुता एवं विस्तारवादी प्रवृत्ति उत्तराखंड के वनों के लिए बड़ी चुनौती है। चीड़ के जंगलों को सुनियोजित तरीके से उपयोगी पेड़ों के जंगल में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है, पर हो इसके उलटा रहा है। चीड़ के जंगल लगातार विस्तार पा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में चीड़ दिखाई नहीं देता था, ये आज वहां तक विस्तार पा चुके हैं।जंगल की आग पर काबू पाने के तौर-तरीकों में नई तकनीकी का प्रयोग जिस गति से होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। ड्रोन का प्रयोग केवल सूचना के त्वरित प्रसार तक ही सीमित है। लीफ ब्लोअर (सूखे पत्रों को हवा से साफ करने वाली मशीन) का उपयोग अभी तक आम नहीं हो पाया है। कृत्रिम बारिश अभी तक सोच के स्तर तक ही है। कुल मिलाकर अंग्रेजों के जमाने से अब तक अगर आग बुझाने का कोई कारगर उपाय दिखता है तो वह है झांपा। झांपा पेड़ों के हरे पत्तों से युक्त टहनियों से बनाया गया बड़ा झाड़ू ही होता है, जिससे दूर से ही खड़े होकर आग बुझाई जाती है।
लेखक वर्तमान में दून विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।