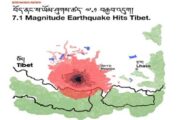देवेन मेवाड़ी
सन् साठ के दशक के अंतिम वर्ष थे। एम.एससी. करते ही दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में नौकरी लग गई। आम बोलचाल में यह पूसा इंस्टिट्यूट कहलाता है। इंस्टिट्यूट में आकर मक्का की फसल पर शोध कार्य में जुट गया। मन में कहानीकार बनने का सपना था। ‘कहानी’, ‘माध्यम’ और ‘उत्कर्ष’ जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं में मेरी कहानियां छपने लगी थीं। समय मिलते ही कनाट प्लेस जाकर टी-हाउस और काफी-हाउस में जाकर चुपचाप लेखक बिरादरी में बैठने लगा था। पूसा इंस्टिट्यूट के भीतर ही किराए के एक कमरे में अपने साथी के साथ रहता था। कभी-कभी इलाहाबाद से प्रसिद्ध लेखक शैलेश मटियानी जी आ जाते थे। हमारे लिए वे जीवन संघर्ष के प्रतीक थे। उनके पास टीन का एक बड़ा और मजबूत बक्सा होता था। जब पहली बार आए तो कहने लगे, “यह केवल बक्सा नहीं है देबेन, इसमें मेरी पूरी गृहस्थी और कार्यालय है। वे मुझे देबेन कहते थे। लत्ते-कपड़े, किताबें, पत्रिका की प्रतियां, लोटा, गिलास, लिखने के लिए पेन, पेंसिल, कागज, चादर, तौलिया, साबुन, तेल, शेविंग का सामान, कंघा, सब कुछ।” कमरे में आकर उन्होंने एक ओर दीवाल से सटा कर बक्सा रखा और बोले, “दरी है तुम्हारे पास?”
मैंने दरी निकाल कर दी। उन्होंने फर्श पर बीच में दरी बिछाई और बोले, “मैं जमीन का आदमी हूं। जमीन पर ही आराम मिलता है। इन फोल्डिंग चारपाइयों पर तो मैं सो भी नहीं सकता।” कमरे में इधर-उधर मेरी और मेरे साथी कैलाश पंत की फोल्डिंग चारपाइयां थीं। उन्होंने बक्सा खोला। उसमें से ब्रुश और पेस्ट निकाल कर बु्रश किया। हाथ-मुंह धोया। मेरे पास पंप करके जलने वाला कैरोसीन का पीतल का स्टोव और पैन था। उसमें चाय बनाई। चाय पीते-पीते बोले, “बंबई जाना है। सोचा, दो-चार दिन तुम्हारे पास रुकता चलूं। यहां भी लोगों से मिल लूंगा।”
वे जितनी देर कमरे में रहते, किस्से सुनाते रहते। इलाहाबाद के, बंबई के, अपने जीवन के, तमाम किस्से। सुबह जल्दी निकल जाते और लहीम-शहीम शरीर लेकर दिन भर पैदल और बसों-रिक्शों में यहां-वहां साहित्यकारों, मित्रों से मिलते, अपनी साहित्यिक पत्रिका ‘विकल्प’ के लिए विज्ञापन जुटाते। इस भाग-दौड़ के बाद थकान से चूर होकर शाम को लौटते। मुझसे बहुत स्नेह रखते थे। एक दिन थके-थकाए लौटे तो दरी में लेट कर बोले, “देबेन, तू मेरा छोटा भाई है। मेरे पैरों में खड़ा होकर चल सकता है?”
मैं और मेरा साथी सुन कर चौंके। उस दिन शायद पैदल बहुत चल चुके थे। मैंने सकपका कर कहा, “इतने बड़े लेखक के शरीर पर मैं पैर रख कर कैसे खड़ा हो सकता हूं?”
“अरे, तुम मेरे छोटे भाई हो। बड़े भाई के पैरों में पीड़ा हो रही है। समझ लो डाक्टर हो, इलाज कर रहे हो। अच्छा चलो, तुम मेरे पैरों में चलते रहो, मैं तुम्हें उस फिल्म की कहानी सुनाऊंगा जिसके प्रोड्यूसर ने मुझे कहानी के लिए एडवांस भी दे दिया था, कुछ हजार रूपए।”
मैं बहुत झिझकते हुए उनके पैरों पर खड़ा हुआ तो बोले, “पैरों को दबाते रहो,” और उन्होंने कहानी शुरू की। कहने लगे, “फिल्म की वह कहानी मैंने अपने उपन्यास ‘हौलदार’ और ‘चिट्ठी रसैन’ को मिला कर लिखनी थी।”
“लिखनी थी माने लिखी नहीं?” मैंने पूछा।
“कहां, बस भाग-दौड़ में ही रहा। फिर बंबई छोड़ कर इलाहाबाद आ गया। कोई बात नहीं, प्रोड्यूसर की रूचि होगी तो अब भी लिख दूंगा।”…
“अच्छा तो सुनो, फिल्म कैसे शुरू होती है। पर्दे पर किसी फौजी के पैर और चमड़े के बूट चलते हुए दिखाई देते हैं, पहाड़ी पथरीली सड़क पर। घसड़क….घसड़क…घसड़क…..एक धार (छोटी पहाड़ी) में आकर पैर थमते हैं। केवल धूल से सने बूट दिखाई दे रहे हैं…..हां देवेन, ऊपर पीठ से होकर गर्दन तक चलो। चलते रहो, शाबाश।”
“तो फिर क्या होता है?”
“फिर कैमरा धीरे-धीरे ऊपर उठता है। फौजी की वर्दी और साइड फेस से होता हुआ कैमरा सामने रुकता है। वहां कांसे का एक बड़ा भारी घंटा लटक रहा है, दो मजबूत खंभों पर। कैमरा घंटे का क्लोज-अप दिखाता है। उस पर उकेर कर लिखा गया है – यह घंटा बाड़ेछीना के ठाकुर खड़क सिंह वल्द गुमान सिंह ने अपने बेटे सूबेदार हयात सिंह के नाम पर इस मंदिर को भेंट किया।….और, इसके साथ ही फौजी का मजबूत गठीला हाथ आगे बढ़ता है, घंटे के राले को पकड़ कर जोर से टकराता है – टन्न्न्!….हां, कंधों पर चलते रहो।”
“उसके बाद कैमरा घूमता है। मंदिर में लटकी सैकड़ों छोटी-छोटी घंटियां और विभिन्न आकार के घंटे दिखाता है। फिर चीड़ के पेड़ों से होकर नीचे नदी किनारे के चौरस खेतों में पहुंच जाता है।”
“यहां फिल्म में हीरोइन गोपुली का प्रवेश होता है। वह अपनी तमाम सहेलियों के साथ मंडुवा (रागी) की पकी हुई फसल के खेतों में खड़ी है। बगल में मादिरा (ज्वार) की फसल पक कर तैयार है। पृष्ठभूमि से पहाड़ी संगीत उभरता है। हीरोइन और उसकी सहेलियों के हाथ में दरातियां हैं। वे इस तरह हवा में हाथ उठा कर…”
कंधों में तो मैं पैर रख कर खड़ा था। हाथ कैसे उठाते? हाथ नहीं उठे तो बोले, “अच्छा अब पैरों पर चलो।” तब उन्होंने दाहिना हाथ उठा कर कहा- इस तरह हवा में दराती के साथ हाथ उठा कर वे गाती हैं….
ओ ओ ओ, आ आ आ!
मंडुवा बाला टिपि दिना कन
मादिरा बाला टिप!”
(मंडुवा की बालियां काट दो ना, मादिरा की बालियां काट दो)
बोले, “ये गीत के टेक की लाइनें हैं। गीत आगे बढ़ता है और बीच में टेक सुनाई देती रहती है- मंडुवा बाला टिपि दिना कन, मादिरा बाला टिप!”
“बस इसी तरह कहानी आगे बढ़ती जाती है। किसी दिन लिखूंगा इसे।…अच्छा, हो गया अब। तुम भी खड़े-खड़े थक गए होगे, “कहते हुए वे उठ कर बैठ गए। बोले, “अब आराम मिल रहा है। असल में आज पैदल बहुत चलना पड़ा। इस दिल्ली में कहीं आना-जाना बड़ा मुश्किल काम है।”