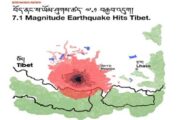विश्वम्भरनाथ साह ‘सखा’
कुमाऊँ में होली के दो प्रचलित स्वरूप है। एक ग्रामीण अंचल की होली, जिसे खड़ी होली कहते हैं। दूसरी, नागर होली, जिसे शहरी क्षेत्रों में बैठ होली कहते हैं। इसे 200-300 वर्ष पूर्व के आस-पास कुमाऊँ में प्रचलित होना माना जाता है। रुहेला आक्रमणों के कारण समय-समय पर मैदानी भागों से लोग कुमाऊँ में आते रहे। विशेष रूप से अल्मोड़ा में राजाश्रय प्राप्त होने के कारण यहीं स्थापित हो गये। इसी क्रम में तवायफों का आगमन व उनके द्वारा प्रस्तुत मुजरों व महफिलों का प्रारूप व राग-रंगों स्मरण मात्र जनमानस में आज भी पूर्ववत बना हुआ है। अतः इसी संदर्भ में बैठ होली आज भी अपना स्वरूप बनाये हुये है।
कुमाऊँ अंचल की बैठ होली की विशेषता यह है कि यह परमात्मा व भक्ति के प्रति अटूट आस्था को प्रतिबिम्बित करती हैं। उदाहरणार्थ पौष मास में इतवारों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अतः पौष मास के प्रथम इतवार से बैठ होली का प्रारम्भ देवस्थल या घरों से प्रारम्भ हो जाता है। यह होलियाँ आध्यात्मिक भाव भूमि में निर्मित होती हैं अतः इन्हें ‘‘निर्वाण’’ होलियाँ कहा जाता है। जैसे :- ‘‘क्या जिन्दगी का ठिकाना, फिरत मन काहे रे भुलाना’’। यह क्रम बसन्त तक चलता रहता है।
इन होलियों की भाषा बृज और खड़ी बोली होती है। इन होलियों में मैदानी भागों में गाई जाने वाली ठुमरी का पूर्ण प्रभाव है। ठुमरी में भी रसीली ठुमरी बनारसी का अंग स्पष्ट रूप से विद्यमान है। गाये जाने वाली होली की अन्तराएं पारसी थियेटर की भंगिमाओं को समेटे हुए होती हैं तथा होली की रचनाएं जब द्रुत लय ग्रहण करती है, तब स्पष्ट रूप से बोल बनाव का निकास नृत्य की भंगिमाएं प्रकट करने लगती है।
ठुमरी का अंग होते हुए भी इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुमाऊँ की होली ठुमरी में प्रयुक्त संकीर्ण राग-रागनियों तक ही सीमित न होकर भारी भरकम रागों में भी गाई जाती हैं। उदाहरणार्थ काफी, खम्माज, धानी, झिझोटी, परज, पीलू, देश, विहाग, विहागड़ा, तिलंग, सिन्दूरा व भैरवी के अतिरिक्त यमन कल्याण, शुद्ध कल्याण, जै- जेवन्ती, शाहना, दरबारी आदि बड़े रागों में भी इन्हें गाया जाता है।
यहाँ की होली गायकी में कुछ अन्य विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। मिश्र खम्माज को यहांँ जंगला काफी कहा जाता है। काफी शुद्ध गाई जाकर मिश्र काफी का प्रचलन मुख्य है। कुमाऊँ में खम्माज के स्वर प्रबल रूप में अधिकांश राग रागनियों में प्रयुक्त किये जाते हैं। रामपुर में जंगला नामक वर्णन मिलता है परन्तु कुमाऊँ की होली में जंगला नाम से गाई जाने वाली होली में खम्माज में आरोह में तीव्र मध्यम -अवरोह में पीलू की भांति कोमल गंधार लगाकर षडज में लाया जाता है।
कुमाउंनी होली की गायकी ठुमरी अंग की बोल बनाव के अंग से सर्वथा भिन्न है। छोटे-छोटे बोलों और उनके बनाव, उनके लगाव की जगह होली गीत की पूरी पंक्ति को अनेक रूप में गाया जाता है और यह क्रम मध्य, मन्द्र व तार सप्तकों में बराबर बना रहता है। ग्रहणीय विशेषता यह है कि कवित्त की पंक्तियों को विभिन्न लयकारियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। स्थाई व अन्तरा में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।
ताल व लय के रूप में कुमाऊँ में होली दो प्रकार से गाई जाती है। एक धमार के नाम से और दूसरी होली के नाम से जानी जाती है। मैदानी भागों में होली का तात्पर्य ही धम्मार माना जाता है तथा यह चौदह मात्राओं का माना जाता है। परन्तु पर्वतीय धम्मार सोलह मात्राओं की होता है। इसमें-धिट, तिट, कित, गधिगिन के बोलों का सम्मिश्रण होता है। एक तरह से धम्मार और चौताल का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। इसे मध्य लय की तीन ताल की लाग से ही बजाते व गाते हैं। अर्थात तीन भरी व एक खाली इसके अतिरिक्त इसमें मात्र दुगुन की ही बढ़त होती है।
दूसरी होली ठुमरी अंग की चांचर ताल में गाई जाती है, जो सोलह मात्रा की होती है तथा इसकी लय मध्य तीन ताल में होती है। इसकी चाल और आस तो दीपचदी की तरह कायम की जाती है, परन्तु खाली व भरी के स्थान चार-चार मात्रा के होते हैं। चांचर ताल का वर्णन लयात्मक विवेचना के अन्तर्गत उत्तर भारतीय संगीत में ‘ताल अद्धा’ जत के रूप में प्रचलित है तथा ठुमरी गायकी में इनका प्रयोग होता है। परन्तु कुमाउंनी बैठ होली में प्रयुक्त चांचर ताल मध्य त्रिताल से थोड़ी नीचे की लय बजाई जाती है। दूसरी विशेषता यह है कि होली के स्थाई और अन्तरे का उठान तीसरी ताली अर्थात पांचवी मात्रा से किया जाता है। ठाठ में जो लय गाई या बजाई जाती है उससे थोड़ी बढ़ी लय में परन्तु दुगुन से कम में तीन ताल बजाई जाती है। तीन ताल के बाद तीन ताल की दुगुन से थोड़ा गिरी हुई लय में कहरूआ बजाया जाता है। स्थाई और अन्तरा गायन इन्हीं क्रमों से गाया व बजाया जाता है। यह एक जटिल पद्धति है, जो शास्त्रीय गायको में भ्रम उत्पन्न करती है। अगर इस क्रम को विलम्बित मध्य व द्रुत गति में विधिवत काल व लय खण्डों में गाने बजाने की योजना बना दी जाय तब उस स्थिति में होली का सशक्त स्वरूप स्थापित होने की पूरी सम्भावना निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होती है।
इसकी गायकी मेंं मध्य लय से प्रारम्भ होकर लगभग दुगन की त्रीताल व इसी लय के कहरूवे तक जाता है। सबसे प्रमुख बात यह होती है कि बोल चाहे स्थाई का हो या अन्तरे का, परन्तु सबका उठान पांचवी मात्रा से ही होता है और कहरूवा भी इसी रूप में तीन भरी व एक खाली ताली के लाग से गाया जाता है तथा तबले में तिये भी इसी के अनुसार लगाये जाते हैं। पर्वतीय बैठ होली में तालों की अभिव्यक्ति के लिये तबला मुख्य वाद्य होता है, परन्तु इसके सहयोगी साजों के अन्तर्गत लोटा व मजीरा मुख्य रूप में दो वाद्य अवश्य होते हैं, जिनके द्वारा खटका लगाया जाता है। दो सिक्कों से उल्टा लोटा बजाया जाता है। यह खटका समां बांधने का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कहावत है कि होली ‘खटकों लटकों’ की होती है। पर्वतीय अंचल की होली की एक विशेषता यह भी होती है कि इसे एकल गायन के अन्तर्गत न रखकर सामूहिक गायन के रूप में समझा जाता है। सामूहिक गायन की वशेष स्वरूप धारणा है। यह कव्वाली अथवा भजन-कीर्तन शैली व लय पर स्थापित होते हुए भी सर्वथा भिन्न है। पर्वतीय बैठ होली में एक गायक स्थाई को गाता है। अनेक रूपों में गाने के बाद दूसरा गायक उसे पकड़ लेता है तथा सजाता-संवराता है फिर तीसरा व्यक्ति उसे उठा लेता है। यही क्रम चौथे या पांचवे अथवा अधिक गायकों द्वारा क्रमानुसार रखा जाता है। तत्पश्चात पुनः मूल गायक उस स्थाई को पकड़ लेता है। इसी प्रकार अंतरा भी गाया जाता है। यही व्यवस्था द्रुत लयोें में भी अपनाई जाती है।
बैठ होली का गायकी स्वरूप रंगमंचीय है। जिस प्रकार पारसी थियेटर में संवाद बोले जाते हैं व विशेष भावों का प्र्रदर्शन अतिरंजना के साथ किया जाता है, उसी प्रकार बैठ होली के कविता भावों का प्रदर्शन-गायन द्वारा संवाद सम्भाषण की तरह किया जाता है। इसमें स्वभाविक रूप से नृत्य की लयात्मकता व मुद्राओं का दर्शन होते रहता है जो श्रोताओं को अतिरिक्त अतिरंजक्ता प्रदान करता है।
पर्वतीय नागर बैठ होली भाव पक्ष पर्वतीय वातावरण या जनमानस में व्याप्त भावाभिव्यक्ति की स्वाभाविक्ता से मेल नहीं खाता और न ठुमरी अंग की भाव-भंगिमाओं के अनुरूप ही बैठता है। उदाहरणार्थ गायी जाने वाली गायन में सुर का लगाव व बोलों की चाल व झोल, पर्वतीय अंचल के लोक संगीत के मूल तत्वोें व लयों से मेल नहीं खाता और न मैदानी क्षेत्रों में गायी जाने वाली ठुमरी के भावों व अभिव्यक्ति की नाना प्रक्रियाओं के अनुरूप होता है। इससे होली मात्र समान स्वरावलियों की पुनरावृत्ति हो कर रह जाती है, भले ही वह एक गायक द्वूरा गाई जाए या क्रमवार कई गायकों द्वारा। परन्तु पर्वतीय बैठ होली अपनी कविता व लयात्मकता अभिव्यक्ति द्वारा एक ऐसा ‘रिदम’ व टैम्पो का निर्माण कर देती है कि सारा श्रोता समूह संकीर्तन की भाव मुद्रा में झूमने लगता है।
आज के युग में भारतीय संगीत में जिस तरह नये प्रयोगों द्वारा नये नये रूपों में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसी प्रकार पर्वतीय बैठ होली में भी प्र्रयोगधर्मिता की आवश्यक्ता है। प्रयोगधर्मिता का ध्येय मात्र चूं-चूं का मुरब्बा बनाना नहीें वरन भाव, स्वर व लय द्वारा मूर्त रूप में इच्छित वातावरण बन पाने की क्षमता का प्रदर्शन होता है।
यहाँ की होली में शहना, काफी, खम्माज, जैजैवन्ती, परज इत्यादि का उदाहरण लेना पर्याप्त होगा। नाम तो पूर्णतः शास्त्रीय लिये जाते हैं, परन्तु वर्ताव तरीके से नहीं किया जाता है। रागों की रचना विशेष स्वर, छन्दों व विशिष्ट शैली द्वारा ही सम्भव होती है और आधार रागांक स्वर छन्द हाते हैं। ठुमरी में राग की शुद्धता नहीं रखी जाती वरन् समवर्ती स्वरां को उस राग में विशेष प्रयोजन से प्रयुक्त किया जाता है, जिससे राग की मूल आत्मा तो सुरक्षित रहे, परन्तु के अनुरूप भाव पक्ष अधिक मूर्त रूप में उजागर हो जाय। परन्तु पर्वतीय अंचल में नताम ‘राग’ का लिया जाता है और उसमें सम्मिश्रण रागां व स्वरों का किया जाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इससे हर राग की चमक व सुगन्ध समाप्त हो जाती है। परन्तु यह स्वीकारना पड़ता है कि पर्वतीय बैठ होली रागों में धुनां का प्रभावकारी स्वरूप निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है।
आज तक पर्वतीय अंचल में बैठ होली जितनी भी व जिस रूप में भी गायी बजायी जाती है, वह मात्र धुन प्रधान है और इसे धुनों का विशिष्ट प्रकार ही माना जा सकता है, भले ही इन धुनों में विज्ञों को विभिन्न राग-रागनियों के स्वर छन्द दिखायी पड़ते हों। अतः होलियों को मात्र होली कहा जाना चाहिये और उसी रूप में गाया बजाना चाहिये। राग व समय की पाबन्दी की बात कहने से विज्ञ संगीत प्रेमियों व साधकों को भ्रम हो जाता है।
आज के युग में भारतीय संगीत में जिसे रूप में नये प्रयोगां द्वारा नाना रूपों को प्रदर्शित किया जा रहा है, उसी प्रकार से पर्वतीय बैठ होली में भी प्रयोगधर्मिता व स्वाराधार की आवश्यक्ता है। इससे एक ओर इसकी विशिष्ट गायकी निखार आएगा तथा दूसरी ओर युवा पीढ़ी वे गायक और वादक जो शास्त्रीय गायन की सिद्धि प्राप्ति की ओर प्रयत्नरत हैं, इस ओर आकृष्ट होंगे। फलस्वरूप नये मिजाज में पर्वतीय होली जनमानस को संगीतानंद की ओर अग्रसारित करेंगी। अन्यथा यह पूर्ववर्ती गायकों, वादकों की अस्पष्ट की परम्परा अन्धकार के गर्त में कहीं खोकर विस्मृत कर दी जाएगी। इसी क्रम में होली विषयक एक उल्लेख करना नितान्त आवश्क है।
कुमाऊँ अंचल में होली गीतों रचना व गायन प्रक्रिया का सतत प्रवाह सैकड़ो वर्षों से चलता रहा है। इसी का परिणाम हैं कि मौखिक रूप से होलियों को सुनकर हर काल की युवा पीढ़ी ने इसे आगे बढ़ाया और नये प्रयासों व लेखन से कालानुसार इसे जन-जन तक पहुँचाया, जिसे आज हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखकर गौरान्वित होते हैं। अतः भूली बिसरी होलियों का संग्रह श्रम साध्य प्रयासों से नैनीताल नगर की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था ‘शारदा संघ’ द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में हस्तलिखित पाण्डुलिपि के रूप में सुरक्षित हैं।
राग पीलू
गजमुख शिव सुत मंगलकारी,
विघ्न हरण गणदेव
लंबोदर तुम मोदक खाओ,
लीला तुमरी नवीन हे दुःख हारी
राग काफी
रार करत घनश्याम गोपिन के संग, करत ठिठोली,
उड़त गुलाल बरसत केसर, रंग विविध नवीन
ऐसी फाग मची आज बृज में, नृत्य करत राधा श्याम
गोपिन संग करत ठिठोली खेलत होली