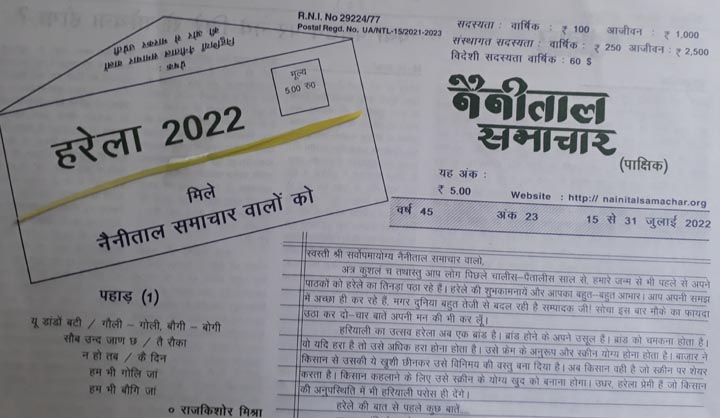राजीव लोचन साह
हरेला सिर्फ पेड़ों और हरियाली का त्यौहार नहीं है, यह मनुष्य को पर्यावरण को लेकर संवेदनशील बनाने की एक कोशिश है। इसी तरह मकर संक्रान्ति को मनाया जाने वाला बच्चों का ‘काले कव्वा’ का त्यौहार उन्हें कौवों या पक्षियों से ही नहीं जोड़ता, प्राणिमात्र के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब यह त्यौहार चलन में आये होंगे, तब हमारे पुरखे प्रकृति के साथ समरस थे। प्रकृति उनके लिये एक साथ रहस्य भी थी और चुनौती भी। मगर प्रकृति को लेकर कोई प्रतियोगिता का भाव या उस पर विजय पाने की इच्छा शायद ही उनके मन में रही हो। यही संस्कार वे अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते थे। बीसवीं सदी की शुरूआत तक यह चलता रहा। फिर विज्ञान और तकनीकी ने लम्बी छलाँगे लगाईं और मनुष्य के मन में भी प्रकृति को जीत लेने और अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की इच्छा हिलोरें मारने लगी। वह उसी दिशा में बढ़ा, बगैर इस बारे में सोचे कि इस कोशिश के साईड एफैक्ट्स क्या होंगे। नतीजा यह हुआ कि सभ्यता तो बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन मनुष्य का अपनी प्रकृति और पर्यावरण से रिश्ता टूटता चला गया। जिन प्राकृतिक तत्वों को लेकर इससे पहले मनुष्य में एक श्रद्धा भाव था, उन्हें वह निहायत उपेक्षा के साथ लेने लगा। प्रकृति ने भी बदला लेना शुरू किया। पर्यावरण से छेड़छाड़ करने के कारण पृथ्वी की ओजोन सतह पर छिद्र होने लगे। जलवायु परिवर्तन अपने दुष्प्रभाव दिखाने लगा। स्थानीय स्तर पर हम पहाड़ में जंगली जानवरों को मेहनत से की गई खेती को नष्ट करते देख रहे हैं। इस अजीबोगरीब समस्या का कि हम अपनी सुख-सुविधायें भी चाहते हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी बन्द नहीं करना चाहते, हम कोई समाधान नहीं ढूँढ पा रहे हैं। हरेला जैसे पर्व को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा और मनाया जाना चाहिये। हम हरेला को सिर्फ कर्मकाण्ड के रूप में न लें, बल्कि उसका मर्म समझें और प्रकृति व पर्यावरण के साथ पुन हमारे पुरखों की तरह समरस होने की कोशिश करें।