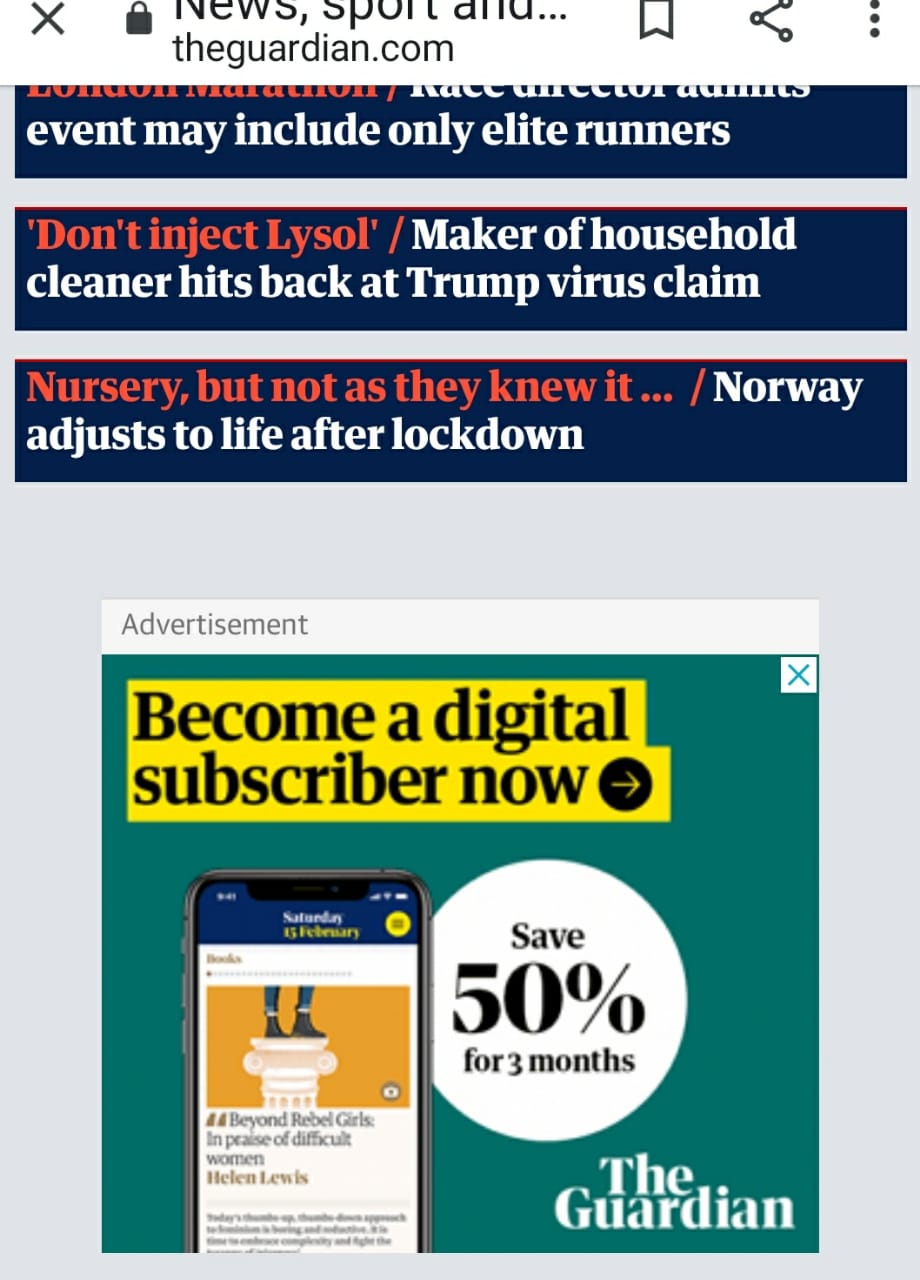भास्कर उप्रेती
जिस दौर में अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप, शशि शेखर जैसे पत्रकार मीडिया का मुखपृष्ठ हो गए हों, ऐसे समय में मीडिया के सशक्त और दीर्घायु होने की कामना करना एक दुविधापूर्ण स्थिति है!
गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी से लेकर गौरी लंकेश तक ने जिस भारतीय मीडिया को गढ़ा-बुना-बनाया उसकी साख का किसी को लाभ मिल रहा है तो वो इन्हीं को मिल रहा है. आखिरकार इनकी आवाज टीवी के पर्दों, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुँचती है. करोड़ों लोगों में से अधिकांश इसे न्यूज़ ही मानते हैं. इनकी बात पर भरोसा करते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं. मगर, यह भी मान लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री के डूबने का प्रभाव इस तरह के पत्रकारों पर नहीं पड़ना है. ये लोग अपने समूहों में शीर्ष पदों पर हैं और कई बार मालिकों की सी हैसियत रखते हैं. इन्हें बड़े पैकेज मिलते हैं. इन्होंने वैध-अवैध स्रोतों से पीढ़ियों के लिए कमा लिया है. मंदी और कोरोना की आंधी के बाद यदि किसी के सर्वाइव करने की गुंजाईश है तो वह भी यही जमात है.
डूबने-उतराने के इस खेल में बौद्धिक श्रम से पत्रकारिता और आजीविका करने वाले हजारों पत्रकार और उनके परिवार गंभीर संकट में आ गए हैं. 25 मार्च को शुरू हुए राष्ट्रीय लॉक डाउन की वजह से अधिकतर पत्रकार घरों में बंद हो गए. प्रिंट पत्रकारों में से बहुत थोड़े पत्रकार दफ्तरों में पहुँच सके. इलेक्ट्रोनिक में भी बहुत कम लोग फील्ड में दिखे. मुंबई जैसे मीडिया-केन्द्रित महानगरों में जहाँ कुछ पत्रकार फील्ड में गए, वहां कोरोना ने उन्हें पकड़ लिया. मुंबई में 53 पत्रकारों के पॉजिटिव मिलने की खबरें आईं हैं, वहीं दिल्ली-लखनऊ जैसे नगरों से भी पत्रकारों के पॉजिटिव मिलने की खबरें आने लगी हैं.
पत्रकारों का काम का काम है सूचनाएं एकत्र करना. इसके लिए बाहर निकलना एक अनिवार्यता है. मगर, कोरोना इसकी इजाजत नहीं देता. वह पत्रकारों को नहीं पहचानता. जो पत्रकार जितना साहसी होगा, उसे ये उतनी ही जल्दी पकड़ लेगा. आधुनिक इतिहास में यह पहली बार है कि पत्रकार न सिर्फ फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि घरों में बैठे रहने पर अधिक असुरक्षित हो उठे हैं. दो विश्व युद्धों, हिरोशिमा-नागासाकी, तमाम गृह युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों के वक़्त ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्रकार असहाय होकर घर बैठ गए हों. घर में बैठे रहने के साथ मानसिक यंत्रणा और अपराधबोध हो ही रहा है, आगे भी हमेशा के लिए घर बैठे रहने की आशंकाएं प्रबल हो उठी हैं.
भारतीय मीडिया बालू के ढेर में खड़ा चमकता हुआ बुर्ज है. कोरोना की आंधी ने इसके नीचे की रेत को उड़ाकर इसे जमींदोज कर दिया है. यह रेत बनी थी विज्ञापनों से. मंदी (जो कि दरअसल महामंदी ही थी, मगर कोई बोल नहीं रहा था) और महामारी के दुर्योग ने विश्व की सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री का दंभ भरने वाले उद्योग का खोखलापन सामने ला दिया है.
आरएनआई के मुताबिक इस समय भारत में 1,18,239 पंजीकृत प्रकाशक हैं. इनमें से 17,573 दैनिक समाचार पत्र हैं, 1,00,666 पीरियोडिकल्स और 900 टीवी चैनल हैं. न्यूज़ चैनल्स में से लगभग 50 प्रतिशत समाचार चैनल्स हैं. टाइम्स ऑफ़ इंडिया ग्रुप विश्व का सबसे बड़ा मीडिया घराना है और ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ अख़बार विश्व का सबसे अधिक प्रसार वाला अंग्रेजी दैनिक. भाषाओं में विश्व में सबसे अधिक प्रसार वाला ‘दैनिक जागरण’ है. उसी के आस-पास खड़ा है ‘दैनिक भास्कर’. चंद समूहों जैसे टाइम्स ग्रुप, एचटी ग्रुप, एक्सप्रेस ग्रुप, दि हिन्दू ग्रुप, टेलीग्राफ आदि को छोड़ दें तो भारतीय मीडिया का बड़ा समूह नव-उदारवाद की आंधी से ही जन्मा है. यानी यह जन्मना ही बाजारू और भ्रष्ट रहा है. यहाँ शराब, खनन, कोयला और प्रॉपर्टी व्यवसाय करने वालों ने मुनाफा और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए निवेश किया है या खुद के मीडिया संस्थान खोल लिए हैं. कई मीडिया संस्थानों के मालिक या शेयरधारकों में राजनेता भी शामिल हैं.
मगर, इतने बड़े घराने कोरोना के पहले ही प्रहार में ढह गए. ये खुद के लिए पूँजी का निर्माण करने वाले पत्रकारों की हिफाजत नहीं कर सके. जिन बड़े घरानों से उम्मीद थी कि वे अपने कर्मचारियों के साथ खड़े होने की स्थिति में हैं उन्होंने ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों से किनारा करना शुरू कर दिया.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया ग्रुप (‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘आज तक’, ‘रेडिओ मिर्ची’ आदि) ने पहले ‘टाइम्स लाइफ’ सप्लीमेंट को मर्ज करते हुए उसके कर्मचारियों की छुट्टी की. फिर ‘संडे मैगज़ीन’ भी बंद कर दी. स्टाफ को संस्थान छोड़ने के मेल कर दिए. बचे हुए कर्मचारियों के वेतन में 5 से 10 फ़ीसदी कटौती की घोषणा कर दी. दूसरी खबर ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘बिजनेस स्टैण्डर्ड से आई’. यहाँ सैलरी कट हुआ. हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप (‘हिंदुस्तान’, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’, ‘कादम्बनी’, ‘नंदन’, ‘रेडिओ फीवर’, ‘दि मिंट’ आदि) ने गजब का खेल किया. सैलरी स्ट्रक्चर में घपला करते हुए फिक्स्ड पे का बड़ा हिस्सा वेरिएबल कंपोनेंट में डाल दिया. साथ ही अपने कर्मचारियों से 25 प्रतिशत तक सैलरी कटौती की अपील कर डाली. जो कहने को वोलंटरी थी लेकिन जिसे असल में सबके लिए लागू ही होना है. पुणे से निकलने वाले ‘साकेत टाइम्स’ ने 15 कर्मचारियों को निकाल दिया. ‘हमारा महानगर’ ने अपने मुंबई, पुणे और नासिक के एडिशन ही बंद कर दिए.
43 साल पुराने अंग्रेजी दैनिक ‘स्टार ऑफ़ मैसूर’ ने बंदी कर ली. ‘न्यूज़ नेशन’ ने 10 पत्रकारों को बाहर कर दिया. बड़े जोशो-खरोस से शुरू हुए ‘क्विंट न्यूज़’ ने अपने टीवी चैनल को बंद कर दिया, साथ ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बिना तनख्वाह के काम करने के लिए कहा. सुभाष चंद्रा (जी ग्रुप) का अख़बार ‘डी.एन.ए.’ बंद कर दिया गया. ‘डेक्क्न क्रोनिकल’ ने केरल संस्करण को बंद कर दिया. ‘दि एशियन एज’ ने मुंबई और कोलकाता संस्करण बंद कर दिए हैं. एनडीटीवी ने 50 हज़ार मासिक से अधिक पाने वालों के लिए 50 प्रतिशत तक पे-कट का एलान किया है. पे-कट तो बाकी प्रिंट और टी.वी. मीडिया ने भी कर दी है, लेकिन सबसे खतरनाक है नौकरी का ही चला जाना.
मीडिया घरानों ने सन्देश दिया कि उनके लिए उनकी कंपनी में सबसे अनुत्पादक कोई चीज है तो वो हैं पत्रकार. सबसे पहले किसी पर गाज गिरेगी तो वह है पत्रकार.
उद्योगों में बंदी और मंदी की वजह से पहले से ही विज्ञापन दरें कम थीं, जब संस्थानों के विज्ञापन विभाग कोरोना से लड़खड़ा गए तो कई संस्थानों ने पत्रकारों पर ही विज्ञापन लाने का दवाब बनाना शुरू कर दिया. मतलब साफ़ है, नौकरी बचानी है तो विज्ञापन जुटाओ. ‘प्रभात खबर’ ने तो पत्रकारों से 25 हज़ार का विज्ञापन लाने या 25 हज़ार जमा करने के लिए कहा. ऐसे में पत्रकार विज्ञापन जुटाने लगे. मगर, छिटपुट विज्ञापनों से इतने विशाल संस्थान कब तक चलेंगे? और विज्ञापन आएंगे कहाँ से? जब विदेशी पूँजी भाग खड़ी हुई है, जब शेयर बाज़ार ब्लड बाथ कर रहे हों, जब सभी बड़े उद्योग बंद हों, छोटे उद्योग अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हों, कौन विज्ञापन देगा? कोई कंपनी विज्ञापन तब देती है जब सामान्य रूप से उसका उत्पाद न बिक पा रहा हो, उत्पाद गोदामों में डंप पड़े हों. कंपनियों की बैलेंस शीट में विज्ञापन देने की गुंजाईश दिख रही हो.
‘दि फाइनेंसियल टाइम्स’ के मुताबिक एतिहासिक रूप से उपभोक्ता बाज़ार की खपत 50 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी है. गर्मी शुरू होते ही कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का जो बाज़ार आसमान छूने लगता था वह लॉक डाउन के बाद भी संभल पाएगा कहना मुश्किल है. कम से कम मई और जून में इनका वही माल बाज़ार में आएगा जो पहले से गोदामों में इंतजार कर रहा है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारतीय मीडिया के लिए एक बड़ा विज्ञापनदाता है, लेकिन उसकी कमर कोरोना के पहले ही टूट चुकी थी, जब 40 प्रतिशत तक सेल गिर गई थीं. नाज़ुक हालातों से गुजर रहे लोग आगे भी कारें खरीदेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं लगता. वही हाल एक बड़े विज्ञापनदाता प्रॉपर्टी सेक्टर का है. यह और भी बुरी हालत में है. यह मीडिया इंडस्ट्री को सहारा देगा या खुद को संभालेगा. हाल के दिनों में उभर रहे टूरिज्म सेक्टर को भी कोरोना ने बड़ा झटका दिया है. लॉक डाउन के कई महीनों या सालों बाद तक यह सेक्टर संभल पाएगा कहना मुश्किल है. भयभीत लोग अब भीड़भाड़ से दूरी, कम ट्रेवल और बाहर खाना खाने से बचेंगे.
मौजूदा समय में ‘सीएनबीसी आवाज’ को छोड़कर एक भी टीवी चैनल मुनाफे में नहीं है. यह एकमात्र चैनल भी बिजनेस न्यूज़ की वजह से मुनाफे में है. वैसे भी मीडिया इंडस्ट्री में सबसे अधिक विज्ञापन-निवेश क्रिकेट और एंटरटेनमेंट चैनलों में हो रहा है. फिलहाल टल चुका आई.पी.एल. इस साल नहीं होता तो यह मीडिया के लिए एक और बड़ा सदमा होगा. टीवी न्यूज़ की कीमत है, केबल या डिश टीवी का रिचार्ज पैक. उपभोक्ता 150 से लेकर 600 रुपए में हजारों चैनल सब्सक्राइब कर सकता है.
1991 के बाद से तेजी से उभरा मीडिया सेक्टर, जो पत्रकारिता के कंटेंट को अपनी पहचान बनाने की बजाय आई.पी.ओ. से खेलने लगा. शराब माफिया और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के दम पर होने वाले इन मीडिया हाउसेज के सालाना जलसे अब इन्हीं को मुंह चिढ़ा रहे.
अख़बार और न्यूज़ चैनल का बाज़ार की कमोडिटी भर में तब्दील हो जाना, अब बाज़ार के नियमों के अधीन उसको ध्वस्त करने को तैयार है. बाज़ार की प्रकृति है अच्छे दिनों की लूट में अपने पार्टनर्स को फलने-फूलने देना और बुरे दिनों में उनकी लुटिया डुबो देना. मीडिया इंडस्ट्री कोई पाक साफ़ इंडस्ट्री नहीं कि बाज़ार के नियम उस पर लागू नहीं होंगे.
पहले अपने बैनर को ब्रांड बनाना, फिर खबर को एक सामान की तरह बेचना, अधिक बिकने वाली खबर का चयन करना, भाषा को बाज़ार के फूहड़ मानदंडों पर ले आना, खबर बेचने वालों को सेलिब्रिटी बनाना, उनके जीवन में महँगी कारों, हवाई यात्राओं का प्रवेश..यब सब उसी का छोटा रूप है जो विजय माल्या के साथ होता हुआ देख रहे हैं. विज्ञापनों के मुनाफे से फूले हुए ये कुप्पा शेर फिलहाल 50 प्रतिशत की कटौती भी झेल सकते हैं, मगर कब तक? और मीडिया इंडस्ट्री में इनकी खुद की तादात कितनी है? जब उत्पाद बनाने में जुटे पड़े फील्ड पत्रकार और फैक्ट्री के प्रोड्यूसर ही पिट जाएंगे तो आका क्या करेंगे? कब तक रंगीन परदों से इतराते रहेंगे? मोटी तनख्वाहें पाकर लाल हुए अनुत्पादक प्रिंट मीडिया के चंद चीफ एडिटर और एग्जीक्यूटिव एडिटर, इन्हें मालिक कब तक झेल सकेगा? जब जहाज में छेद ढूँढने-उसकी मरम्मत करने वाले कामगार ही नहीं रहेंगे तो पानी यहाँ से आए या वहां से जहाज डूबना तय है.
हो सकता है कुछ दिन सरकार से दाना-पानी मिल जाए. मगर, इस दौर में सरकार यह अपव्यय करने की स्थिति में है? सरकार उसको खुश करना चाहती है या उसे बैलेंस करना चाहती है, जो अकड़ के सामने खड़ा हो. जब मीडिया उद्योग का 99 फ़ीसदी हिस्सा पहले से ही पी.आर. एजेंसी की भूमिका में हो तो उसे क्यों सरकारी धन लुटाना है. यदि सरकार को ही मीडिया इंडस्ट्री को पालना पड़ जाए, तो फिर मीडिया का वजूद रहेगा कहाँ? ऐसा मीडिया कोई भी ऐसी खबर नहीं बनाएगा और चलाएगा जो सरकार को नापसंद हो. इस तरह की भूमिका सस्ते आईटी सेल अच्छे से निभा लेंगी.
आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि एक विषाणु के प्रहार से, जिसकी भारत में आहट अधिक है, प्रकोप कम. विश्व की सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री की प्रतिरोधक क्षमता कहाँ गुल हो गई? विश्लेषक कहते हैं कि इसने अपने ही ग्राहक को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था. मीडिया का काम था- पाठक का सशक्तिकरण. लेकिन, इसने उसे अपने मुनाफे के अनुकूल (वह फिर चाहे नागरिक की, संविधान की, मूल्यों की धज्जियाँ ही क्यों न उड़ाने वाला हो) खबरें बनाना शुरू कर दिया. मुनाफा हुआ, मगर मुनाफा तो नशा भी होता है. नशे की जद में आए मीडिया मुगलों को यह गलफहमी हो गई कि हम पाठक या दर्शक के दम पर नहीं चलते. पाठक की खिल्ली उड़ाते हुए कुछ मीडिया-मैनेजर यह तक कह रहे थे कि हम तो उसे मुफ्त में पढ़ाते हैं, या मुफ्त में दिखाते हैं. मगर, दे क्या रहे थे? मुफ्तखोरी की लत. अब जब आप डूब रहे हो तो वह बेचारा क्यों आपके साथ खड़ा हो? बल्कि उसने तो आपके प्राइम टाइम को घटिया इंटरटेनमेंट घोषित करते हुए शुद्ध मनोरंजन वाले चैनलों का रुख कर लिया था.
ऐसे भारतीय मीडिया इंडस्ट्री की मौत पत्रकारिता की मौत नहीं है. यह मुनाफाखोरों की मौत है. जरूर मौत के इस अंधे कुएँ में कई श्रमजीवी पत्रकार गिरकर पिस रहे हैं. उन्हें अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे अपने बच्चों की महँगी फीस जमा करनी होगी, उन्हें कार की इएमआई ज़मा करनी होगी, घर की किश्त भरनी होगी, पता नहीं और क्या-क्या मंसूबे जो बांधे होंगे. चिंता सता रही है कि पता नहीं कब एच.आर. से मेल आ जाएगी? वेतन में कटौती की होगी या नौकरी छूट जाने की? छोटे शहर या गाँव से जहाँ से भी वह आया था कभी पत्रकार बनने, अब लौटकर पत्रकार नहीं जाएगा. वहां टीवी देखने वाले लोग जानते हैं, यह मसखरों का एक घटिया शो था.
तब क्या है भारत में पत्रकारिता का भविष्य?
यह जरूर होगा अब कि जितने चैनल या प्राइम टाइम बचे रहेंगे वह सरकार और तानाशाह के यशोगान से भरे मिलेंगे. सरकार जब तब जरूरत होगी उन्हें पालेगी, बल्कि सरकार भी अब मसखरों की छंटनी करेगी. अच्छे मसखरे और ख़राब मसखरे. सही निवेश का ख़याल सरकार भी रखेगी. पत्रकारों में से जो थोड़े से पत्रकार बच गए हैं या जिस पत्रकार के अन्दर थोड़ी सी भी पत्रकारिता बची रह गई है, वह अपनी राह बदल लेंगे.
तब क्या भारतीय पत्रकारिता की आत्मा का जागरण होगा?
शायद पत्रकारों में से जो पत्रकार बाहर निकलेंगे या जो अभी भविष्य के गर्भ में पत्रकार ही बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, वह कुछ अलग करेंगे. हो सकता है वे सोच पाएं कि पत्रकारिता को खबरों के ही दम पर खड़ा किया जाना चाहिए. वैसे भारत के सन्दर्भ में यह कहना बहुत मुश्किल है. अगर, ऐसा होना हो तो भी इसमें कितना वक्त लगेगा, बताना और भी मुश्किल है. क्यूंकि हमारा यानी पाठक का मुफ्तखोर मिजाज भी कोई कम कोरोना नहीं है.
बावजूद इसके भारतीय पत्रकारिता जगत में कुछ मद्धम मद्धम लौ मौजूद है. खासकर, मुख्यधारा की पत्रकारिता से उक्ता गए या मार भगाए गए चंद पत्रकार. डिजिटल मीडिया में उन्हें सुनने के लिए लोग भीड़ जमा रहे हैं. हालाँकि, भीड़ को देखकर किसका मन कोका कोला हो जाए कहना मुश्किल नहीं. डिजिटल मीडिया एक नई दुकान है. अभी अधिक लोकतान्त्रिक और अधिक स्वायत्त दिखने वाली. हालाँकि, इससे कमा सकने की कुंजी बड़े कोर्पोरेट ने पहले से ही अपने हाथ में रख ली है. वह अभी आपके हिट्स देख रहे हैं, कल आपका कॉन्टेंट भी तय कर सकते हैं. या पुराने अनुभवों की मदद से आपको पूरा खरीद सकते हैं. लेकिन, आने वाले कुछ वर्षों तक तो इसकी धूम मचनी तय है. पिछले एक-डेढ़ महीने के कोरोना काल में डिजिटल मीडिया की जबरदस्त वकत रही. चल ही रही है. कुछ पत्रकारों ने, कुछ गैर-पत्रकार पत्रकारों ने यहाँ पढ़े जाने और देखे जाने के झंडे गाड़ दिए. इनमें से कितने पत्रकारों की जेब में पैसा गया, यह अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन, डिजिटल लिटरेसी की कमी, यहाँ आए कंटेंट को कमतर या नया मानने की गलतफहमी से बहुत कम ने पैसा बनाया होगा, यह तय है.
यह भी साफ़ है कि इसी दौर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम जैसी कंपनियों ने चाँदी काट ली. टीम्स, ब्लू जींस, मीट, क्लासरूम, हैंग आउट आदि ऑनलाइन भेंट करवाने वाली या वर्क फ्रॉम होम कराने वाली एप्स ने अपनी संभावनाओं की जोरदार भविष्यवाणी कर दी है. यदि दुनिया कोरोना के सबक के बाद संभलती है तो यह तकनीक नया मीडिया उभरकर आएगा. इसी दौर में जिओ जैसी एकाधिकारवादी संचार कंपनियों ने अपनी पकड़ भी कहीं गहरी कर ली है.
पारंपरिक पत्रकारिता रहेगी ही नहीं?
उसका जवाब तो है- कि लगभग हाँ. एक-दो अख़बार, एक-दो टीवी चैनल पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए किसी तरह शायद सर्वाइव कर जाएँ. अपनी जमा-पूँजी के दम पर थोड़े साल और जोखिम उठा ले जाएँ. मगर, क्यूंकि पूँजी का बुलबुला अभी शांत है. अमीर मुल्क संरक्षणवादी नीतियों की ओर मुड़ रहे. वे अपनी सीमाओं से फैले कॉरपोरेशंस को डोमेस्टिक निवेश के लिए मजबूर करेंगे. आने वाले दिनों में देशी पूँजी और राष्ट्रवाद की अधिक सघन दोस्ती तय है, ऐसे में जनता की आवाज उठाने वाले माध्यम इन्हीं की इच्छाओं के भरोसे हो जाएंगे. भारतवर्ष नामक देश में तो कई मीडिया समूह एक ही पूँजी-स्रोत की छतरी के नीचे पहले से आ रहे हैं, आने वाले दिनों में यह ध्रुवीकरण अधिक तेज होगा. भारतीय मीडिया का कोरियाई मॉडल विकसित होगा और यह ‘प्रावदा’, ‘चाइना डेली’, ‘शिन्हुआ न्यूज़’ से बुरी गत को प्राप्त होगा.
मगर यदि आशावादी रुख रखें तो उसकी भी थोड़ी जगह तो है. पिछले दिनों में ‘दि हिन्दू’ ने अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा दी थी. वह भी उस समय जब ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ ने अपना चेन्नई संस्करण बड़े जोर-शोर से लांच किया.
ऐसा माना जा रहा था कि ‘दि हिन्दू’ आज गया-कल गया. लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से यह नहीं हुआ. ‘दि हिन्दू’ का सर्कुलेशन घटने की बजाय थोड़ा बढ़ गया. समूह ने तय किया है कि वह अपने कॉन्टेंट की कीमत माँगेगा. यदि पाठक कीमत देकर खरीदने को राजी हुए तो ठीक, वर्ना वह एक सम्मानजनक मौत मरेगा. इस सब के बीच अख़बार के मौजूदा पाठकों ने कीमत देकर इसे खरीदने का विकल्प ही चुना है. यह एक सकारात्मक घटना हो सकती है, जहाँ से बाकी मीडिया भी कुछ सीख सकता है. ‘दि हिन्दू’ ने अपने ई-संस्करण को भी सब्सक्राइब करने की अपील की है. सीमित अर्थों में वेबसाइट अभी फ्री है, लेकिन लिमिटेड कंटेंट के साथ. समूह ने यह भी तय किया है कि वह बड़ा मीडिया घराना बनने की बजाय कॉन्टेंट बेस्ड पत्रकारिता करना पसंद करेगा. यदि हिन्दू का यह प्रयोग सस्टेन करता है तो यहाँ से भारतीय मीडिया के विज्ञापन आधारित मौजूदा मॉडल से मुक्त होने की राह खुलेगी.
वैश्विक परिदृश्य क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने वैभव और चमक की वजह से रुपर्ट मर्डोक जैसे बाजों का शिकार पहले से ही है. ‘डेमोक्रेसी नाउ’ जैसे प्रो-पीपल इलेक्ट्रोनिक माध्यम दुनिया में अपवादस्वरूप ही हैं. मगर, जिन अख़बारों की उम्र 100, 150 या 200 साल की हो चुकी. जो अब ब्रांड, मीडिया हाउस की बजाय अख़बार की स्टीरियोटाइप छवि के साथ ही स्वीकार किए जाते हैं- जैसे ‘दि गार्डियन’, ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘दि वाल स्ट्रीट जर्नल’, ‘अल डियारिओ’, ‘योमिउरी शिमबन’, ‘ले मोंड’ आदि. ये संस्थान अपनी स्वतंत्र एंटिटी बनाने की कोशिश में हैं. विकसित देशों से निकलने वाले इन अख़बारों में से किसी के पास सरकारी या प्राइवेट विज्ञापनों का कोई अकाल नहीं था. इन्हें जो बात अच्छे से पता थी वो था पूँजी का परिवर्तनशील चरित्र.
2017 तक ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ की स्थिति वही थी, जो आज के ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ की है. ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ करीब 48 पेज (जिसमें 25-28 पेज विज्ञापनों को समर्पित होते हैं) का छपता है. एक अख़बार छापने में करीब 12 रुपए खर्च आता है. मगर, पाठक को यह मिलता है 1 से 4 रुपए के बीच में. यानी अख़बार सर्कुलेशन के दम पर उतना कमाता है जितना कि हाकर को देना होता है. यदि अख़बार किसी चौराहे में रख दिए जाएँ तो तब यह खर्च भी न आए. महंगी रंगीन स्याही, ग्लॉसी पेपर, मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट, पत्रकारों की पगार इसका अख़बार की बिक्री से कोई संबंध नहीं है. इसी तरह की गत हुई ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ की. यह चौराहों, कॉफ़ी हाउसों, मेट्रो स्टेशनों, अस्पतालों, पार्कों या पुस्तकालयों में दयालु पाठकों की दया-दृष्टि चाहता. मगर, इस एतिहासिक और सम्मानित अख़बार को लोग लुग्दी ही मानने लगे. अख़बार कुछ दिन सनसनी-न्यूज़ छापने की फिराक में रहा तो कभी कोर्पोरेट को खुश रखने की जुगत में. मगर, अख़बार को लोग अख़बार की तरह लेने को राजी न हुए. यह अमरीकी पत्रकारिता पर सबसे गंभीर तंज था.
अख़बार की साख गिरी तो न सिर्फ विज्ञापनदाताओं ने दुत्कारा, बल्कि सरकार भी इसका मखौल उड़ाने लगी. परिणामत: अखबार गंभीर घाटे में आ गया. अंतत: अखबार के तत्कालीन कारकुनों ने तय किया कि अखबार को अखबार बनाने पर ही फोकस किया जाए. कम लेकिन हाई क्वालिटी कॉन्टेंट. पाठक से सीधे-सीधे अपनी बात रखेंगे. हम नागरिक के लिए अच्छा अखबार निकाल रहे हैं, क्या नागरिक एक अच्छा अख़बार पढ़ना चाहेगा? अख़बार ने प्रिंट, ऑनलाइन और वीडिओ संस्करण की कीमत तय कर दी. यह बहुत कम थी, नाममात्र की. सौदा पाठकों को पसंद आ गया. एक साल के सघन अभियान के बाद अख़बार न सिर्फ मुनाफे में आ गया, आज भी है, बल्कि उसका रीडर्स बेस भी बढ़ गया. किसी संस्थान में काम कर रहे पत्रकारों के लिए इससे अधिक सम्मान की बात नहीं हो सकती कि उसका उपभोक्ता उसके माल को न सिर्फ कीमत देकर खरीदे, बल्कि उस पर भरोसा भी करे.
इसी के समानांतर लगभग बंद ही हो चुके ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने भी नई राह चुनी. हालाँकि यह थोड़ा विवादस्पद है, लेकिन फ़िलहाल इसका अख़बार के अख़बार होने पर प्रभाव नहीं पड़ा है. अख़बार के अधिकांश शेयर अमेजन ने खरीद लिए. अमेजन ने इसे घाटे का सौदा कहते हुए इसलिए खरीदा क्यूंकि उन दिनों अखबार ने पत्रकारिता की स्थिति पर व्यंग्य करते हुए यह स्लोगन चलाना शुरू किया था- ‘डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस’. बहरहाल अमेजन और पोस्ट के बीच यह समझौता काम कर रहा है कि अख़बार का कॉन्टेंट निवेशक कंपनी के इन्टरेस्ट से प्रभावित नहीं होगा. यह भी अच्छी बात रही कि पिछले दो सालों ने ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने अपना उपभोक्ता वर्ग वापस हासिल कर लिया है, अखबार खरीदने के लिए चुकाई जा रही कीमत पर.
ब्रिटेन से प्रकाशित ‘दि गार्डियन’ की कहानी अधिक प्रेरक हो सकती है. 2017 में इस पर 57 मिलियन यूरो डॉलर का कर्ज था, अपनी नीति में बदलाव लाते हुए यह एक ही साल में 800 हज़ार यूरो डॉलर के मुनाफे में आ गया. अख़बार ने व्यापक स्तर पर अपने पाठकों से प्रोडक्ट की कीमत देकर पढ़ने की अपील की और खबरों की गुणवत्ता को पेशेवराना मानकों पर उतारा. यह अख़बार ऑनलाइन फ्री पढ़ा जा सकता है. जहाँ एक अपील साथ-साथ रहती है कि हम पत्रकारिता कर रहे, मुनाफे का व्यवसाय नहीं. इस अपील का यह असर हुआ कि ‘गार्डियन’ का सब्सक्रिप्शन बेस्ड रीडर न सिर्फ यूरोप में बढ़ा, बल्कि पूरी दुनिया में उसके पाठक तैयार हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया में गूगल और फेसबुक को तय करना पड़ा है कि वहां पत्रकारों-लेखकों के कॉन्टेंट का उन्हें पे किया जाएगा.
बहरहाल, भारतीय मीडिया की स्थिति अभी बेहद संक्रमणशील है. यहाँ लोकतंत्र या नागरिक चेतना की अमरीकी, यूरोपीय या जापानी परंपरा नहीं है. हम वैसे ही हैं जैसे हमारे पड़ोसी भाई पकिस्तानी हैं. मीडिया इंडेक्स में कभी वे हमसे दो अंक ऊपर हो जाते हैं, कभी हम. हम दोनों देश मीडिया की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के सवाल पर निचले पायदानों पर ही बने हुए हैं. हमारे यहाँ जरूर खुद्दार पत्रकारों के कुछ नाम मिल जाएंगे, मगर यहाँ मजबूत मीडिया संस्थान कभी नहीं रहे. 2014 से पहले जब थोड़ा अधिक कहने की गुंजाईश थी, तब भी मीडिया का प्रभावशाली वर्ग सत्ता की ओर ही झुका रहता था; आज वह बुरी तरह उसके चरणों में नतमस्तक है. मीडिया कर्मियों का नेतृत्व करने वाले एक संगठन ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स’ की एक मिमियाती अपील से भारतीय मीडिया इंडस्ट्री की हैसियत समझी जा सकती है. जब संगठन ने एक मीडिया समूह द्वारा मीडियाकर्मियों की छंटनी न करने और सरकार से इसमें हस्तक्षेप की अपील की तो उधर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक फरमान बाहर आ गया. फरमान था आकाशवाणी और दूरदर्शन में एक दशक से अधिक समय से काम कर रहे कैजुअल वर्कर्स को बाहर निकालने का. इसके बाद तो एक के बाद एक मीडिया संस्थानों में होड़ मच गई अपने वर्कर्स को बाहर निकालने या उनकी सैलरी कट करने की.
जाहिर है ये स्थितियां लोकतंत्र के भविष्य को और अंधकारमय बनाएंगी. आज का मीडिया ख़राब है लेकिन आर्थिक संकट से गुजरने के बाद वह अधिक ख़राब होगा. उसमें आम जन की आवाज को उठाने की शक्ति और क्षीर्ण हो जाएगी, तय है. कोरोना ने हमें चेताया है कि मीडिया संस्थान का अपने पाठकों के बलबूते खड़ा रहना कितना जरूरी है. यदि पाठक किसी सामान की कीमत चुकायेंगे तो जाहिर है उसकी क्वालिटी बेहतर बनाए रखने के लिए भी सचेत रहेंगे. चेक एंड बैलेंस की इसी स्थिति से भारतीय मीडिया अपनी सही शक्ल में आ सकेगा.