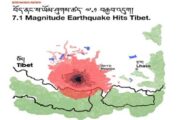सबसे पहले कुलपति भौतिकी विभाग में गये। यह वह विभाग है, जिसे कुमाऊँ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. डी. डी. पन्त ने स्थापित किया था। इस जगह काम करने की ऐसी ललक उनमें थी कि जब तक उनके हाथ-पाँव चलते रहे, वे इस विभाग में शोध कार्य करते रहे।
8 दिसम्बर की प्रातः दस बज कर दस मिनट पर कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डी. के. नौड़ियाल एकाएक, बगैर किसी पूर्व सूचना के नैनीताल स्थित डी.एस.बी. कैम्पस के मुख्य द्वार पर पहुँचे। वहाँ पर उन्हें गणित के प्राध्यापक डॉ. एम. सी. जोशी अपने स्कूटर से उतरते हुए दिखाई दिये। डाॅ. जोशी ने हाथ जोड़ कर उनका अभिवादन किया तो ‘‘चलिये, डाॅ. साहब आज कैम्पस का एक राउण्ड लेते हैं,’’ कहते हुए कुलपति महोदय ने उन्हें अपने साथ ले लिया। कैम्पस निदेशक प्रो. एल. एम. जोशी उस रोज छुट्टी पर थे।
उसके बाद अगले सवा घंटे तक कुलपति डाॅ. नौड़ियाल ने जो देखा, उससे उन्हें भले ही हैरानी हुई हो, कुमाऊँ विश्वविद्यालय को नजदीक से जानने वालों के लिये वह सामान्य बात है। साढ़े ग्यारह बजे तक, जब कुलपति वापस स्लीपी होलो स्थित अपने प्रशासनिक भवन को वापस गये, अधिकांश विभागों के ताले भी नहीं खुले थे। सबसे पहले कुलपति भौतिकी विभाग में गये। यह वह विभाग है, जिसे कुमाऊँ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. डी. डी. पन्त ने स्थापित किया था। इस जगह काम करने की ऐसी ललक उनमें थी कि जब तक उनके हाथ-पाँव चलते रहे, वे इस विभाग में शोध कार्य करते रहे। रिटायरमेंट के सालों बाद तक भी। एक बार उन्होंने मुझ से कहा भी था, ‘‘राजीव, एक वक्त था जब दुनिया के अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालयों में जाने के मौके मेरे पास थे। मगर इस जगह का मोह मुझसे छूटा नहीं। इस विभाग का और नैनीताल शहर का।’’
मगर शुक्रवार 8 दिसम्बर की सुबह इस विभाग के बस ताले खुल पाये थे। लैब या कमरों में कोई नहीं था। कुलपति चौंके। उसके बाद वे रसायन विभाग में पहुँचे। सौभाग्य से वहाँ प्रयोगशाला में भी काम हो रहा था, पढ़ाई भी चल रही थी और अधिकतर अध्यापक भी मौजूद थे। कुछ ग़ैरहाज़िर रहे भी होंगे तो वे कुलपति की जानकारी में नहीं आये। इसके बाद कुलपति न्यू आर्ट्स ब्लाॅक में गये, जहाँ कला संकाय के सारे विभाग अवस्थित हैं। हर जगह उन्हें ताले लटके हुए मिले। सिर्फ अंग्रेजी विभाग में संविदा पर काम करने वाली एक अध्यापिका मिली, जिसने कुलपति को बताया कि हालाँकि उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, मगर तब भी वह हमेशा समय पर आ जाती है। भूगोल विभाग में कुलपति को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी मिला, जिससे रजिस्टर माँग कर कुलपति ने बाकायदा उसमें स्टाफ की अनुपस्थिति अपने हाथ से दर्ज की।
डी.एस.बी. परिसर में दूसरा विभाग जहाँ शिक्षण कार्य चल रहा था, गणित विभाग था। हालाँकि कुछ शिक्षक तब तक भी नहीं आये थे। मगर कुल मिला कर यह आभास होता ही था कि यह एक जीवन्त विश्वविद्यालय का हिस्सा है।
उल्लेखनीय बात यह थी कि कुलपति को परिसर में विद्यार्थी ठीक-ठाक संख्या में मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे पढ़ने आये हैं, मगर अध्यापक तो अक्सर आते ही नहीं। कम से कम कक्षा के समय तो नहीं आते।
अत्यन्त बेआबरू होकर, सवा घंटे परिसर में टहल कर कुलपति डाॅ. डी. के. नौड़ियाल वापस चले गये।
इस घटना के ठीक एक सप्ताह पूर्व 1 दिसम्बर को डी.एस.बी. परिसर में कुमाऊँ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कुलपति प्रो. डी. के. नौड़ियाल ने डॉ.. महेन्द्र सिंह पाल (पूर्व सांसद), एडवोकेट मोहन चन्द्र पांडे और प्रो. देब सिंह कार्की के साथ मुझे एक शाॅल ओढ़ा कर सम्मानित किया। वजह थी हमारा 1972 के ‘विश्वविद्यालय आन्दोलन’ का एक सिपाही होना। अपना नाम पुकारे जाने पर मैं बहुत चैंका। अब आप किसी कार्यक्रम में मौजूद हों और आपको मंच पर बुलाया जाये तो उद्घोषणा की अवज्ञा कर न जाना पूरे कार्यक्रम में अराजकता उत्पन्न कर देता है। अतः थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मैं गया, मैंने कुलपति से बूके लिया, विनम्रतापूर्वक शाॅल पहना और फिर थोड़ी धृष्टता के साथ उद्घोषक डाॅ. ललित तिवारी के हाथ से माईक छीन लिया। वे कहते रह गये कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपनी बात रखने के लिये आमंत्रित करूँगा। मैंने कहा कि बाद में नहीं, मैं अभी ही बोलूँगा। अपने बेहद संक्षिप्त वक्तव्य में मैंने कहा कि यह सम्मान लेते हुए मुझे बेहद अटपटा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड राज्य आन्दोलन का श्रेय कुछ व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, उसी तरह विश्वविद्यालय स्थापना आन्दोलन का श्रेय भी कुछ व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिये। डॉ. महेन्द्र सिंह पाल एक अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि वे 1971 में देब सिंह बिष्ट महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। मैंने कहा कि मैं यह सम्मान उन सैकड़ों विद्यार्थियों की ओर से ही ग्रहण कर सकता हूँ, जिन्होंने 1966 से 1972 तक मेरे साथ डी.एस.बी. में शिक्षा पायी। विश्वविद्यालय आन्दोलन की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मैंने कहा कि मूलतः यह आन्दोलन गढ़वाल में दक्षिण से आये संन्यासी स्वामी मन्मथन की पहल पर शुरू हुआ, जिसे गढ़वाल के प्रबुद्ध और जागरूक लोगों का समर्थन मिला। फिर कृष्णानन्द मैठाणी, वीरेन्द्र पैन्यूली और अवध बिहारी पन्त जैसे उस वक्त के तमाम युवा भी इस आन्दोलन से जुड़े। अल्मोड़ा छात्रसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और उनके साथियों के द्वारा इसे कुमाऊँ में विस्तार मिला। आन्दोलन तेज हुआ तो पिथौरागढ़ में पुलिस के गोली चलाने पर दो लोगों की मृत्यु भी हुई। फिर बातचीत का लम्बा दौर चला और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने इस आशंका के चलते कि कहीं कुमाउनी और गढ़वालियों में सिर न फूट जायें, एक पर्वतीय विश्वविद्यालय के स्थान पर दो, कुमाऊँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय बना दिये। अन्त में मैंने कहा कि चवालीस साल बाद पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय ने भी हमारे सपने उसी तरह तोड़े, जिस तरह उत्तराखंड राज्य ने तोड़े हैं।
ठीक एक सप्ताह बाद मेरी बात की कुलपति के औचक निरीक्षण से पुष्टि हो गई।
उस रोज स्थापना दिवस समारोह में मेरे बाद तमाम वक्ताओं ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की खूब चर्चा की। सिर्फ कुलपति नौड़ियाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय हम चले तो सही रास्ते पर थे, मगर अधबीच में न जाने कब और कहाँ पर रास्ता भटक गये। उस समारोह की पोस्ट मैंने फेसबुक पर लगाई तो मुझे इतनी कम प्रतिक्रियायें मिलीं कि मुझे विश्वास हो गया कि जिस तरह लोगों ने उत्तराखंड राज्य की नियति को स्वीकार कर लिया है, उसी तरह कुमाऊँ वि.वि. की नियति को भी स्वीकार कर लिया है।
एक छात्र, एक पत्रकार, एक आन्दोलनकारी और एक नागरिक के रूप में तो मैंने कुमाऊँ विश्वविद्यालय को निकट से देखा ही। मैं विश्वविद्यालय कार्य परिषद् का एक सत्र के लिये सदस्य भी रहा। एक भ्रष्ट कुलपति के साथ मैंने तीन साल काटे और अगली बार कार्य परिषद् के चुनाव में ‘मृतकों’ द्वारा वोट दिये जाने के मुद्दे पर पहले चरण, विश्वविद्यालय कोर्ट, का चुनाव जीतने के बावजूद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तत्कालीन कुलाधिपति मार्गरेट अल्वा ने मेरी शिकायत पर कोई भी कदम उठाने से इन्कार कर दिया था। कार्य परिषद् में काटे तीन साल मेरी जिन्दगी के सबसे निकम्मे साल थे। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस विश्वविद्यालय को बचाने का कोई सीधा या सरल तरीका नहीं हो सकता। जब सारे ही पक्ष, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारी और क्षेत्र की सारी जनता एकजुट हो कर संघर्ष नहीं करते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मगर लगता नहीं कि इनमें से दो पक्ष, अध्यापक और कर्मचारी, जिनके भारी भरकम वेतनमान अब आँखें चैंधिया देते हैं, अपनी खेमेबाजी से मुक्त हो कर कुछ करने को उत्सुक भी हैं।