राजीव लोचन साह
उत्तराखंड में पंचायत चुनावों का एक मंजर अभी-अभी हमने देखा है। जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। किस तरह से हमारे जन प्रतिनिधि बिक रहे हैं, किस तरह सैर-सपाटा कर रहे हैं, हमारे जिम्मेदार मीडिया ने रस ले लेकर सब कुछ तफसील से बताया है। इस मामले में मीडिया ने उस तरह से ‘थोड़ा सा दिखाने और ज्यादातर छिपाने’ की वह नीति भी छोड़ दी है, जो केन्द्र में मोदी सरकार के आने के बाद उसने अपना ली है। ज्यादातर लोग ऐसी खबरें पढ़-सुन कर बहुत खुश हैं। राजनीति में अनैतिकता के इस कीचड़ में हम कितना गहरे धँस गये हैं, इस ओर उनका ध्यान भी नहीं जा रहा है। उन्हें यह सब सामान्य लग रहा है, जैसे यह रोजमर्रा की चीज हो। यह ऐसा ही होता है, इसे ऐसा ही होना चाहिये। किसी तरह का गुस्सा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि यह अफसोस में सिर पीटने का मामला है।
जिस विकेन्द्रित शासन व्यवस्था को हम देश और प्रदेश की मुक्ति के सबसे कारगर औजार के रूप में देखते हैं, उसने सरकारी पंचायती व्यवस्था के रूप में हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि काले धन का जिस बड़े पैमाने पर इन चुनावों में प्रयोग हुआ है, उसके बाद पंचायतों के लिये चुने गये जन प्रतिनिधि ईमानदारी से अपना काम करेंगे ? वे इन चुनावों में किये गये आर्थिक निवेश को तथाकथित विकास के लिये पंचायतों में आने वाली धनराशि में से वसूल नहीं करेंगे ? इस धनराशि का पिच्चासी प्रतिशत लूट-खसोट में नहीं लगेगा ?
हाँ, यही कहा था हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया था कि केन्द्र सरकार से जो एक रुपया गाँवों के विकास के लिये भेजा जाता है, वह गाँवों तक पहुँचते-पहुँचते 15 पैसे रह जाता है। और तभी 73वें-74वें संविधान सशोधन कानूनों के रूप में दो बेहद क्रांतिकारी कानून पारित हुए थे। 73वाँ संशोधन कानून ग्राम पंचायतों के लिये और 74वाँ कानून नगर निकायों के लिये। 25 साल से अधिक हो गया है इन कानूनों को लागू हुए, मगर इन्हें प्रदेश सरकारों ने अपने-अपने प्रदेशों में लागू करना है। वे इन्हें लागू नहीं करतीं, क्योंकि तब पूरे का पूरा एक रुपया गाँव में लग जायेगा। खाने-पीने के लिये क्या बचेगा ? शुरू में कुछ प्रदेशों में यह कानून लागू करने की कोशिश की गई थी। बहुत अच्छे परिणाम निकलने भी लगे थे। मगर फिर एक रुपये में से 85 पैसे डकार लेने वालों के दबाव में इन्हें छोड़ दिया गया। अब तो राजनीति के संदर्भ में यह एक वर्जित विषय हो गया है। बड़ा ताज्जुब है कि इन पच्चीस सालों में हम सेक्स के मामले में तक बेहद खुला हुआ समाज हो गये हैं। मगर 73वाँ-74वाँ संविधान संशोधन कानून के बारे में चर्चा करना इस समाज में निषिद्ध हो गया है।
महात्मा गांधी भारत को आठ लाख गाँवों का गणराज्य बनाना चाहते थे। मगर सत्ता हाथ में आते ही उनके उत्तराधिकारियों ने इस विचार को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वह तो भला हो राजीव गांधी का कि उन्होंने उपरोक्त कानूनों के जरिये पंचायतों और शहरी निकायों को सांवैधानिक हैसियत दी। अब संसद, विधान सभायें और पंचायती राज संस्थायें बराबर की हैसियत रखती हैं। जैसी संसद वैसी ही ग्राम सभा। वहाँ प्रधानमंत्री है तो यहाँ ग्राम प्रधान। मगर वैसा हो कहाँ रहा है ? ग्राम प्रधान तो पंचायत सचिव के घर पर उसके जूठे बर्तन मल रहा है, उसका बस्ता ढो रहा है और बदले में उससे पंचायतों से खाने-कमाने के तरीके सीख रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी सचिव के घर पर उसके बर्तन मलेगा ? क्या आपने कभी इस सम्भावना पर कभी सोचा कि जो जिलाधिकारी आज खुदा न सही, खुदा से थोड़ा ही कम है, उसकी हैसियत इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष के सचिव की जैसी हो जायेगी। यानी सारे निर्णय जिला पंचायत करेगी और डी.एम. उन्हें अमली जामा पहनायेगा। पूरी सच्चाई तो यह है कि आज के ये जिले, जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी सरकार के लिये राजस्व बटोरने के लिये बनाया था, खत्म हो जायेंगे और विकास के लिये नये जिले बनेंगे। मैं जगह-जगह ‘अलग जिला बनाओ’ की माँग करने वालों को यही सलाह देता हूँ कि यह माँग छोड़ो और 73वाँ-74वाँ संविधान सशोधन कानून लागू करने की माँग करो, क्योंकि इनमें आजादी के बाद पहली बार ‘जिला’ शब्द का उल्लेख किया गया है। जिस तरह आजादी के बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, वैसे ही हर प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन किया जायेगा। क्योंकि अब रेवेन्यू विलेज नहीं विकास के जिले बनने हैं। देश को उस प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, जिसमें एक बार हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर अगले पाँच सालों तक हमें लूटते रहने के लिये उसे निगरगंड छोड़ देते हैं, से सहभागिता मूलक लोकतंत्र, जिसमें हर गाँव, हर मोहल्ले का निवासी यह तय करेगा कि उसका विकास कैसे होना है, की ओर बढ़ना है। क्या आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि जरूरत तो आपके निकट एक हाईटेक शौचालय की थी, मगर सांसद निधि या विधायक निधि से गली में टाईल्स लगा दिये गये, जबकि गली तो अभी ठीकठाक थी, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी।
यह सांसद और विधायक निधियाँ क्या हैं ? जन प्रतिनिधियों को पूरी तरह ठेकेदार बना देने की व्यवस्था। जैसे इसके बगैर वे ठेकेदारी करते ही नहीं! सारा उत्तराखंड तो इन 19 सालों में ‘ठेंकेदार खंड’ बन कर रह गया है। नरसिंहाराव ने अपनी अल्पमत सरकार को सत्ता में रखने के लिये एक तरीका ढूँढा था एमपीलैड यानी सांसद निधि के जरिये एकजुट रखने का। फिर वह निधि विधायकों तक भी आ गयी। जिन जन प्रतिनिधियों को ‘लाॅ मेकर’ यानी ‘कानून निर्माता होना चाहिये था, वे सदन में बहस करना भूल कर कानूनसम्मत ढंग से ठेकेदार बन गये। विधान सभा, जहाँ साल में कम से कम दो सौ दिन बैठ कर उन्हें बहस करनी चाहिये थी, जनता के हित में कानून बनाने चाहिये थे, वह साल में बीस दिन भी नहीं चलती और विधायक अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और कारिन्दों को ठेके बाँटते फिरते हैं। ऊपर से पेंशन भी खाते हैं। यही है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र!
73वाँ-74वाँ संविधान सशोधन कानून में जिला नियोजन समिति के माध्यम से आप अपनी जिला योजना बनाते हैं। हर ग्राम सभा, हर नगर निकाय अपनी जरूरतें, अपनी प्राथमिकता तय कर उस योजना में शामिल करता है और फिर वह राज्य वित्त आयोग के पास पहुँचती हैं, जहाँ से उन्हें इस योजना के लिये धन मुहैया करवाया जाता है। बेशक राज्य सरकार के माध्यम से, मगर राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता, क्योंकि वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। जिलाधिकारी, सी.डी.ओ., बी.डी.ओ. जैसी परतें भी खत्म हो जाती हैं और एक रुपया पूरे का पूरा पंचायत तक आ जाता है। राज्य सचिवालय से लेकर विकास भवनों तक पर्दे के पीछे जो खेल होते हैं, वे खत्म हो जाते और यदि जनता थोड़ी जागरूक हो, अपने चुने हुए प्रधान पर कड़ी नजर रखे तो भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो सकता है।
ऐसी शिकायतें खत्म हो जायेंगी कि हमारे इलाके में शराब की दुकान क्यों खुली या हमारी यह जमीन फलाँ उद्योग को क्यों दे दी गई। ग्राम सभा के अधिकारों का अतिक्रमण तो फिर केन्द्र सरकार भी नहीं कर सकती। आखिर अब ग्राम सभा की सांवैधानिक हैसियत संसद से कम जो क्या है ? अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है ? ग्राम सभा बनायेगी। डाॅक्टर-अध्यापक नहीं हैं ? कोई बात नहीं। ग्राम सभा स्वयं डाॅक्टरों-अध्यापकों को नियुक्ति देगी। ग्राम सभा का अपना कैडर होने के कारण ये डाॅक्टर-अध्यापक कहीं जा भी नहीं सकेंगे, जब तक इस्तीफा न दें या ग्राम सभा उन्हें निकाल न दे। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है। कोई बात नहीं। ग्राम सभा, विकास खंड और जिला पंचायत के आपसी तालमेल से वह भी दुरुस्त हो जायेगी। जैसे एक राज्य की बसें दूसरे राज्य में जा सकती हैं। जिले के भीतर आवागमन उसी तरह आसान हो जायेगा। हर ग्राम सभा या नगर निकाय अपनी सीमा के भीतर सड़कें बना सकते हैं, विकास खंड स्तर पर या जिला स्तर पर उनकी देख-रेख हो सकती है। आखिर जिला नियोजन समिति के पास यह अधिकार भी तो है कि वह जिले के भीतर प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विभिन्न विकास खंडों या ग्राम सभाओं-नगर निकायों के बीच होने वाले विवाद सुलझा सके।
यह सब कुछ एक मायालोक जैसा लगता है, नहीं ? मानो अलादीन का चिराग मिल गया हो। लेकिन यदि हम 73वाँ-74वाँ संविधान संशोधन कानून के नजरिये से देखें तो ये सारी बातें कतई असम्भव नहीं हैं। संविधान के अन्तर्गत यह एक ऐसा तरीका ऐसा है जिससे जनता अपनी किस्मत खुद बदल सकती है। जितना आप 73वाँ-74वाँ संविधान संशोधन कानून के अन्तर्गत घुसेंगे, देखेंगे कि देश की ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसे ये सुलझा न सकती हों। मगर ऐसा हो कहाँ रहा है? विकास के नाम पर लूट-खसोट को जारी रखने के लिये पचास साल पुरानी सड़ी-गली पंचायती राज व्यवस्था चलाई जा रही है, जिसमें 73वाँ-74वाँ संविधान संशोधन कानून से लेकर कुछ रंग-रोगन कर दिया गया है। खूब लूट हो रही है। हमारा पैसा हमसे ही छीना जा रहा है। लूटने के लिये दिल्ली-मुम्बई से वे लोग आ रहे हैं, जिनका गाँव से रिश्ता भी टूट गया है। मगर पैसे के दम पर वे प्रधानी झपट लेते हैं। साल में बीस दिन भी इलाके में न रहने वाले, स्थायी रूप से हल्द्वानी-देहरादून में रहने वाले लोग इलाके के जन प्रतिनिधि होने का दम भरते हैं।
हमारे इस दुर्भाग्य को मीडिया मजे ले लेकर हमें बता रहा है और हम खुश हैं। अरे, हम 73वाँ-74वाँ संविधान संशोधन कानून को समझें तो और फिर छीन कर अपना हक लें। इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है।
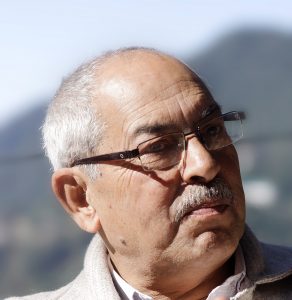
राजीव लोचन साह 15 अगस्त 1977 को हरीश पन्त और पवन राकेश के साथ ‘नैनीताल समाचार’ का प्रकाशन शुरू करने के बाद 42 साल से अनवरत् उसका सम्पादन कर रहे हैं। इतने ही लम्बे समय से उत्तराखंड के जनान्दोलनों में भी सक्रिय हैं।



































